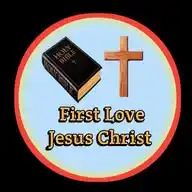Mazdoor Bigul मजदूर बिगुल www.mazdoorbigul.net
2.1K subscribers
About Mazdoor Bigul मजदूर बिगुल www.mazdoorbigul.net
'मज़दूर बिगुल' देश की उस 80 करोड़ मेहनतकश आबादी की आवाज़ है जिन तक मुख्यधारा के मीडिया की निगाहें कभी पहुँचती ही नहीं। यह इस देश के मेहनतकशों की ज़िन्दगी, उनके सपनों और संघर्षों की तस्वीर पेश करता है, और मेहनतकशों, संवेदनशील युवाओं और जागरूक नागरिकों के सामने इस दमघोंटू अन्यायपूर्ण सामाजिक ढाँचे का विकल्प पेश करता है, अपने हक़ों के लिए लड़ने और जीतने के लिए ज़रूरी ज्ञान और समझ से उन्हें लैस करने की कोशिश करता है। पूँजीवादी मीडिया की लीपापोती और पर्देदारी को भेदकर यह देश और दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण आर्थिक-राजनीतिक-सामाजिक घटनाओं का बेबाक विश्लेषण प्रस्तुत करता है और निराशा के बादलों को चीरकर उम्मीद और हौसले की रोशनी दिखाने वाली साहित्यिक और वैचारिक कृतियों से उन्हें परिचित कराता है। अगर आप हर महीने 'मज़दूर बिगुल' प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो आप इस महादेश के अतीत, वर्तमान और भविष्य के बेहद ज़रूरी पहलुओं को जानने से ख़ुद को वंचित कर रहे हैं।
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

📮__________________📮 *हिंसा-अहिंसा के मिथक-यथार्थ और संगठित हिंसा के विविध रूप* ✍शशिप्रकाश http://www.mazdoorbigul.net/archives/11821 _______________________ *समाज में बढ़ती हिंसा का सामाजिक संरचना से क्या रिश्ता है? इसे समझने के लिए हिंसा और अहिंसा के सवाल पर थोड़े व्यापक संदर्भो में चर्चा जरूरी है।* *दार्शनिक-वैचारिक स्तर पर हिंसा रक्तपात का समानार्थी शब्द नहीं है। किसी भी प्रकार के दबाव या बल-प्रयोग को हिंसा की श्रेणी में रखा जा सकता है।* सत्य का आग्रह (सत्याग्रह) भी यदि हृदय-परिवर्तन या नैतिक विवशता पैदा करने के बजाय भौतिक, विवशता पैदा करता है तो उसमें हिंसा अंतर्निहित है। अंग्रेजों ने भारत नैतिक विवशता या हृदयपरिवर्तन के कारण नहीं, बल्कि ठोस भौतिक विवशता के कारण छोड़ा था, अहिंसा की जो गांधी की अवधारणा थी, स्वयं वे भी उसकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। गांधीवादी आंदोलन ने (और साथ ही तमाम जनसंघर्षों ने तथा वस्तुगत परिस्थितियों ने) अंग्रेजों को विवश किया, न कि उनका हृदय-परिवर्तन किया। *सभी ऐतिहासिक-सामाजिक परिवर्तनों में, प्रत्यक्ष या परोक्ष हिंसा की, हेराल्ड लास्की के शब्दों में, हिंसा या हिंसा के तथ्य’ की भूमिका रही है। शासक वर्ग ने जनसंघर्ष के दबाव के बिना कभी भी सत्ता नहीं छोड़ी है।* पुराण कथाओं में भी तपस्या, वैराग्य और हृदय-परिवर्तन के प्रसंग केवल व्यक्तिगत मुक्ति के संदर्भ में ही आते हैं। सामाजिक स्तर पर न्याय-अन्याय के बीच के फैसले निर्णायक हिंसात्मक संघर्षों से ही होते दिखते हैं। *समस्या तब पैदा होती है, जब व्यक्तिगत हिंसा और भीड़ की हिंसा तथा सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर संगठित हिंसा के बीच फर्क नहीं किया जाता। व्यक्तिगत हिंसा प्रतिक्रियात्मक होती है या रुग्ण सामाजिक परिवेश की देन होती है। भीड़ की हिंसा भी प्राय: अंध प्रतिक्रिया या सामाजिक परिवेश में व्याप्त निराशा-निरुपायता की विस्फोटक अभिव्यक्ति होती है।* भीड़ की हिंसा का सुनियोजित-संगठित इस्तेमाल कई बार अपने निहित राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए फासीवादी या अन्य धुर प्रतिक्रियावादी ताकतें करती हैं। सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर संगठित हिंसा एक सर्वथा अलग चीज है और मुख्यतः इसके दो रूप होते हैं। *संरचनागत हिंसा* *सामाजिक-राजनीतिक स्तर पर संगठित हिंसा का सर्वोपरि रूप अपने आप में राज्य सत्ता है। यह शासन करने वाले लोगों की शासितों के खिलाफ हिंसा या बल-प्रयोग का केंद्रीय उपकरण है, शासक वर्ग की हिंसा का मूर्त रूप है।* बुर्जुआ राज्य सत्ता इन अर्थों में सर्वाधिक परिष्कृत होती है। अपने सांस्कृतिक-वैचारिक उपकरणों से बुर्जुआ वर्ग जन समुदाय को तैयार करता है कि वह शासन करने के उसके विशेषाधिकार को स्वीकार करे। यही वर्चस्व (हेजेमनी) की राजनीति है। पर जनता के प्रतिरोधों का निर्णायक तौर पर दमन बल-प्रयोग या हिंसा के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन राज्य सत्ता की संगठित हिंसा को मात्र यही एक रूप नहीं होता। समाज के तृणमूल स्तर तक राज्य सत्ता के जिन अंगोंउपांगों की पहुंच होती है, उनके नित्य प्रति के कार्य-व्यापार में हिंसा का तथ्य अंतर्निहित होता है। जिलाधिकारी से बी.डी.ओ. तक, पुलिस अधीक्षक से दारोगा तक, पूरी नौकरशाही रोजमरे का काम भय और बल-प्रयोग का सहारा लिये बिना पूरा ही नहीं कर सकती। सरकार से लेकर गांव के प्रधान तक पर भी यही बात लागू होती है। यानी बात केवल जनसंघर्षों के दमन और ‘आर्म्ड फोर्सेज (स्पेशल पॉवर्स) एक्ट’ जैसे काले कानूनों की ही नहीं है। बुर्जुआ राज्य-मशीनरी की रोजमरे की कार्रवाई में हिंसा अनिवार्यतः निहित होती है। इसे बुर्जुआ राज्य सत्ता की संरचनागत हिंसा (स्ट्रक्चरल वाइलेंस) कहा जा सकता है। इससे अलग पूंजीवादी सामाजिक-आर्थिक ढांचे की संरचनागत हिंसा की चर्चा भी जरूरी है। एक अध्ययन के अनुसार भारत की ऊपर की दस प्रतिशत आबादी के पास कुल परिसंपत्ति का 15 प्रतिशत इकट्ठा हो गया है, जबकि नीचे की 60 प्रतिशत आबादी के पास मात्र दो प्रतिशत है। ऊपर की तीन प्रतिशत आबादी और नीचे की 40 प्रतिशत आबादी की आमदनी के बीच का अंतर आज 60 गुना हो चुका है। देश के 0.01 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनकी आमदनी पूरे देश की औसत आमदनी से दो सौ गुना अधिक है। दूसरी ओर, अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन के अनुसार देश के 77 प्रतिशत लोग रोजाना 20 रुपए से भी कम पर गुजर करते हैं। 11 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हैं और 11 करोड़ फुटपाथों पर सोते हैं। 35 करोड़ लोग अल्पपोषण के शिकार हैं, जिन्हें प्रायः भूखे पेट सोना पड़ता है। 75 प्रतिशत मांओं को भरपेट भोजन नहीं मिलता। आधे भारतीय बच्चे कुपोषण से और 60 प्रतिशत रक्ताल्पता से ग्रस्त हैं। देश की सारी तरक्की का फल 1 अरब 20 करोड़ की आबादी में से ऊपर के 20-25 करोड़ लोगों तक ही पहुंच पाता है। इस विपन्न देश का 75 लाख करोड़ रुपए का काला धन स्विस बैंकों में जमा है। नेताओं के भ्रष्टाचार और विलासिता की कोई सीमा नहीं है। ऐसे तथ्यों से पन्ने के पन्ने रंगे जा सकते हैं। ये सभी तथ्य और आंकड़े पूंजीवादी सामाजिक आर्थिक ढांचे में अंतर्निहित संरचनागत हिंसा की उस प्रक्रिया को दर्शाते हैं, जो दिन-रात निरंतर जारी रहती है। *संरचनागत हिंसा का एक और रूप है, जो सामाजिक-सांस्कृतिक मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं के ताने-बाने में गुंथा-बुना होता है। इसके सर्वाधिक प्रातिनिधिक उदाहरण के तौर पर स्त्री उत्पीड़न और दलित उत्पीड़न को लिया जा सकता है। इन मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं को किसी आमूलगामी सर्वतोमुखी सामाजिक परिवर्तन का वेगवाही झंझावात ही तबाह कर सकता है।* बुर्जुआ राज्य सत्ता जब बलपूर्वक यथास्थिति को बनाए रखती है तो प्रकारांतर से वह इन प्रतिगामी मूल्यों-मान्यताओं-संस्थाओं की संरचनागत हिंसा की निरंतरता को भी बनाए रखती है (भले ही प्रकट तौर पर वह इनके विरोध में कानून बनाती है)।। अत: कहा जा सकता है, कि संगठित हिंसा का सर्वोच्च रूप, बलप्रयोग का सर्वाधिक संगठित उपकरण बुर्जुआ राज्य सत्ता होता है। जनता को लगातार बताया जाता है कि राजकीय हिंसा, हिंस न भवति’ और राज्य सत्ता की संगठित हिंसा के प्रत्यक्ष एवं संरचनागत रूपों को दृष्टि-ओझल कर दिया जाता है। राज्य सत्ता की संगठित हिंसा की प्रतिरोधी प्रतिकारी शक्ति क्रांतिकारी संगठित हिंसा होती है। अतीत के दास विद्रोहों और किसान विद्रोहों पर भी यह बात किसी हद तक लागू होती है। अमेरिका और फ्रांस की महान बुर्जुआ जनवादी जनक्रांतियों ने अपनी लक्ष्य प्राप्ति के लिए बड़े पैमाने पर संगठित क्रांतिकारी हिंसा का सहारा लिया था। बीसवीं शताब्दी के सभी राष्ट्रीय मुक्ति संघर्षों में क्रांतिकारी हिंसा या बल-प्रयोग की प्रत्यक्ष या परोक्ष भूमिका थी। बुर्जुआ राज्य सत्ता की संगठित हिंसा इतिहास में सर्वाधिक संगठित है और इसका प्रतिकार जनसमुदाय अपनी सारी शक्तियों को व्यापकतम स्तर पर, कुशलतम ढंग से और सूक्ष्मतम रूपों में संगठित करके ही कर सकता है। जनता द्वारा संगठित क्रांतिकारी, हिंसा या बल प्रयोग का सहारा लेना एक ऐतिहासिक अनिवार्यता होती है। जनता द्वारा बल-प्रयोग राज्य सत्ता द्वारा बल-प्रयोग का प्रतिकार होता है। बल द्वारा स्थापित एवं बल द्वारा संचालित सत्ता को बल द्वारा ही विस्थापित किया जा सकता है। यह गति का ऐतिहासिक नियम है, किसी व्यक्ति की इच्छा नहीं। *पूंजीवादी जनवाद में भी हिंसा* हिंसा की परिभाषा यदि बल-प्रयोग के रूप में करें तो इतिहास में नए युग, नई सामाजिक व्यवस्था और नई सभ्यता-संस्कृति के जन्म की प्रक्रिया में बल की भूमिका हमेशा से प्रसव कराने वाली दाई की और लालन-पालन करने वाले धाय की रही है। यह एक मिथ्या प्रचार है कि क्रांतिकारी हिंसा की बात केवल मार्क्सवादी करते हैं। पूंजीवादी जनवाद के सिद्धांतों को अमेरिका और फ्रांस की महान क्रांतियों सहित यूरोप की जिन क्रांतियों ने मूर्त रूप दिया, वे गृहयुद्धों और बलात् सत्ता-परिवर्तन से भरी हुई थीं। इन क्रांतियों को बुर्जुआ सिद्धांतकार भी महान बतलाते हैं, लेकिन हिंसा की अनिवार्यता पर बल देने का आरोप मार्क्सवादियों पर लगा देते हैं। क्रांतिकारी हिंसा की अनिवार्यता को बुर्जुआ क्रांतियों के महानायकों ने भी समझा था। मार्क्सवाद केवल इतिहास की इस गति का व्यापक संदर्भो में सूत्रीकरण करता है। *समस्या तब खड़ी होती है, जब आतंकवाद और क्रांतिकारी हिंसा के बीच के अंतर को नहीं समझा जाता। मार्क्सवाद के जन्म के पहले से ही, इतिहास में ऐसे क्रांतिकारी मौजूद थे, जिनका विश्वास जन क्रांतियों में नहीं था और जो मानते थे कि थोड़े से चेतना-संपन्न क्रांतिकारी हथियार उठाकरे, षडयंत्र और आतंक के द्वारा, व्यवस्थापरिवर्तन का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।* फ्रांसीसी क्रांतिकारी और कल्पनावादी कम्युनिस्ट लुई ओग्यूस्त ब्लांकी इस धारा का अग्रणी प्रतिनिधि था। रूसी अराजकतावादी बकूनिन के विचार भी इसी धारा के निकट थे। उन्नीसवीं शताब्दी के नौवें दशक में रूसी नरोदवादी आंदोलन की एक धारा (नरोदनाया वोल्या) ने उदारपंथी सुधारवाद का विरोध करते हुए राजनीतिक संघर्ष की आवश्यकता पर बल दिया, लेकिन अपने मध्यवर्गीय नजरिए के कारण वह षडयंत्र और व्यक्तिगत आतंक को ही राजनीतिक संघर्ष का पर्याय मान बैठी। मार्क्स-एंगेल्स और लेनिन ने जनक्रांतियों में अंतर्निहित संगठित क्रांतिकारी हिंसा के तथ्य को तो स्वीकार किया, लेकिन आतंकवादी हिंसा को उन्होंने हमेशा ही विरोध किया तथा उसे निरर्थक एवं हानिकारक बताया। इसके बावजूद, कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर समय-समय पर कभी सुधारवादी भटकाव, तो कभी आतंकवादी भटकाव विभिन्न रूपों में सिर उठाते रहे हैं। कम्युनिस्ट आंदोलन के भीतर से पैदा होने वाले आतंकवादी भटकाव को ‘वामपंथी दुस्साहसंवाद भी कहा जाता है। | क्रांतिकारी आतंकवाद एक मध्यवर्गीय क्रांतिकारी प्रवृत्ति है। पूंजीवाद के दबाव से त्रस्त मध्यवर्ग का विद्रोही हिस्सा व्यवस्था परिवर्तन तो चाहता है, लेकिन उत्पादनप्रक्रिया से प्रत्यक्ष जुड़ाव नहीं होने के कारण उत्पादक मेहनतकश वर्गों की सामूहिक चेतना की जागृति, लामबंदी और सक्रियता में उसका भरोसा नहीं होता। फलतः वह व्यापक जनसमुदाय को जागृत करने के बजाय, तुरत-फुरत क्रांति कर डालने की उद्विग्नता में गुप्त हथियारबंद दस्तों की सशस्त्र कार्रवाइयों और षडयंत्रों का रास्ता अपनाता है। वह व्यापक जनता की तैयारी के बिना, अपने बूते पर जनमुक्ति की लड़ाई लड़ने निकल पड़ता है। वह सोचता है कि हथियारबंद कार्रवाइयों से उत्साहित होकर जनता उठ खड़ी होगी। क्रांतिकारी आतंकवादी हिंसा भी संगठित हिंसा होती है, पर वह मुट्ठी भर लोगों की हिंसा होती है, न कि व्यापक जनसमुदाय द्वारा संचालित हिंसा। व्यापक जनता जब अपनी आर्थिक मांगों और राजनीतिक अधिकारों के लिए संगठित होकर आंदोलनों में उतरती है, उस समय से ही वह शोषकों के विरुद्ध अपनी सामूहिक शक्ति के दबाव और बल-प्रयोग का इस्तेमाल करती हैं। यानी हिंसा का तथ्य हर जनांदोलन में अंतर्निहित होता है। इन आंदोलनों के विरुद्ध आतंक, मुकदमे, लाठीगोली आदि के रूप में राज्य सत्ता संगठित राजकीय हिंसा का इस्तेमाल करती है। संगठित जनशक्ति इसका विविध रूपों में बल-प्रयोग (धरनाप्रदर्शन, टैक्सबंदी, असहयोग, हड़ताल आदि) द्वारा प्रतिकार करती है। यह इतिहास का स्वयंसिद्ध तथ्य है कि निर्णय वर्ग शक्तियों के खुले-उग्र टकराव के सामरिक संघर्ष में रूपांतरण के बाद ही होता रहा है। इनका रूप गृहयुद्ध और जनविद्रोह का भी होता रहा है और दीर्घकालिक लोकयुद्धों का भी, या फिर दोनों का मिला-जुला भी। कई बार व्यापक जनविद्रोह की आसन्नता को देखते हुए शासकों ने सत्ता छोड़ दी। इस प्रक्रिया में रक्तपात भले न हुआ हो, पर क्रांतिकारी हिंसा या बले-प्रयोग का तथ्य अंतर्निहित है। *आतंकवाद बनाम सशस्त्र जनक्रांति* *क्रांतिकारी आतंकवादी हिंसा जनक्रांतियों की संगठित क्रांतिकारी हिंसा से सर्वथा अलग चीज है। फांसी से पहले, जेल में गहन अध्ययन करते हुए भगतसिंह भी क्रांतिकारी आतंकवादी हिंसा की निष्फलता को समझ चुके थे।* अपने आखिरी महत्वपूर्ण दस्तावेज में क्रांतिकारी कार्यक्रम का नया मसौदा पेश करते हुए आतंकवाद की आलोचना की थी और सशस्त्र जनक्रांति की ऐतिहासिक अपरिहार्यता को स्वीकार करते हुए इसके लिए मजदूरों-किसानों की व्यापक आबादी को संगठित करने पर बल दिया था। क्रांतिकारी आतंकवाद के अतिरिक्त प्रतिक्रियावादी, धार्मिक कट्टरपंथी आतंकवाद भी संगठित आतंकवादी हिंसा का एक रूप है। आज ऐसे कई संगठन अमेरिका साम्राज्यवाद का विरोध करते हैं, लेकिन वे सेक्युलरिज्म, जनवाद और समाजवाद के भी उतने ही विरोधी हैं। ये धुर प्रतिक्रियावादी फासिस्ट ताकतें हैं, जो हर स्तर पर विज्ञान और प्रगति का विरोध करती हैं और वर्तमान की पूंजीवादी आपदाओं से निजात पाने के लिए धर्म और अतीत को अपना अंतिम शरण्य बनाती हैं। ये ताकतें वस्तुतः साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की ही भस्मासुर हैं। | महत्वपूर्ण बात यह है कि *आतंकवाद – अपने क्रांतिकारी और प्रतिक्रियावादी, दोनों ही रूपों में, साम्राज्यवाद और पूंजीवाद की दमनकारी राज्य सत्ताओं की प्रतिक्रिया है।* राजकीय आतंकवाद सभी आतंकवादों की जननी होती है। राज्य सत्ता की संगठित और संरचनागत हिंसा ही समाज में अराजक हिंसा (व्यक्तिगत हिंसा और भीड़ की हिंसा) और संगठित आतंकवादी हिंसा के विविध रूपों को जन्म देती है। राज्य सत्ता की संगठित हिंसा का प्रतिकार संगठित जनशक्ति की संगठित क्रांतिकारी हिंसा द्वारा ही किया जा सकता है। आतंकवाद ऐसी किसी जनक्रांति की संगठक शक्ति की अनुपस्थिति, कमजोरी या विफलता के कारण फलता-फूलता है। साथ ही, वह गतिरोध और विपर्याय के अंधकार में निराशा और दिशाहीन विद्रोह की भी एक अभिव्यक्ति होता है। *मार्क्सवाद निरपेक्ष रूप में हिंसा का महिमामंडन कदापि नहीं करता। वह हिंसा की विरुदावली नहीं गाता। अपने अंतिम लक्ष्य के तौर पर वह हिंसा या किसी भी रूप में किसी नागरिक के विरुद्ध बल-प्रयोग का विरोधी है। पर हिंसा या बल-प्रयोग के जरिए कायम सत्ता-संरचना और समाज-संरचना को ध्वस्त करने के लिए वह हिंसा या बलप्रयोग की ऐतिहासिक आवश्यकता को स्वीकार करता है।* इस तरह, सामाजिक बदलाव में संगठित क्रांतिकारी हिंसा की भूमिका को वह ऐतिहासिक-दार्शनिक स्तर पर स्वीकार करता है। मार्क्सवाद एक वर्गविभाजित, हिंसा-आधारित सामाजिक ढांचे में न्यायपूर्ण हिंसा और अन्यायपूर्ण हिंसा के बीच, अल्पसंख्यक उत्पीड़कों की दमनकारी हिंसा और बहुसंख्यक उत्पीड़ितों की प्रतिकारी हिंसा के बीच, अंतर करने पर बल देता है। इसलिए, निरपेक्ष अर्थों में यदि कोई मार्क्सवादियों को हिंसा का पुजारी’ कहता है तो वह अश्लील ढंग से मार्क्सवाद का विकृतिकरण ही करता है। लोकमत समाचार, दीपावली विशेषांक 2010 से साभार ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🖥 प्रस्तुति - Uniting Working Class 👉 *हर दिन कविता, कहानी, उपन्यास अंश, राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक विषयों पर लेख, रविवार को पुस्तकों की पीडीएफ फाइल आदि व्हाटसएप्प, टेलीग्राम व फेसबुक के माध्यम से हम पहुँचाते हैं।* अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इस लिंक पर जाकर हमारा व्हाटसएप्प चैनल ज्वाइन करें - http://www.mazdoorbigul.net/whatsapp चैनल ज्वाइन करने में कोई समस्या आए तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख कर भेज दें - 8828320322 🖥 फेसबुक पेज - https://www.facebook.com/mazdoorbigul/ https://www.facebook.com/unitingworkingclass/ 📱 टेलीग्राम चैनल - http://www.t.me/mazdoorbigul हमारा आपसे आग्रह है कि तीनों माध्यमों व्हाट्सएप्प, फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ें ताकि कोई एक बंद या ब्लॉक होने की स्थिति में भी हम आपसे संपर्क में रह सकें।

📮__________📮 *In Memory of Comrade Che Guevera* _A Spanish song - Hasta Siempre_ https://youtu.be/Y8ynNRN_MxQ ____________ English lyrics given below Until Always [English] We learned to love you from the heights of history with the sun of your bravery you laid siege to death Chorus: The deep (or beloved) transparency of your presence became clear here Commandante Che Guevara Your glorious and strong hand fires at history when all of Santa Clara awakens to see you Chorus You come burning the winds with spring suns to plant the flag with the light of your smile Chorus Your revolutionary love leads you to a new undertaking where they are awaiting the firmness of your liberating arm Chorus We will carry on as we did along with you and with Fidel we say to you: Until Always, Commandante! Chorus Greek version - https://youtu.be/eQlFWidNFWw

📮_______________📮 *What is Israel? इज़राइल क्या है?* ✍️ Renata Em की अंग्रेजी पोस्ट का AI अनुवाद। मूल अंग्रेजी पोस्ट नीचे है। An AI Hindi translation of post by Renata Em Original English post is given below Hindi text -------------- मैं इज़राइल हूँ। मैं हिंसा करते हुए भी पीड़ित होने का दावा करने का कोई मौका नहीं छोड़ता। 1947 में, संयुक्त राष्ट्र ने मुझे किसी और की आधी से ज़्यादा ज़मीन दे दी। एक ऐसा उपहार जो मैंने कमाया नहीं था, उन औपनिवेशिक शक्तियों से जो उसकी मालिक नहीं थीं। मैंने इसे स्वीकार कर लिया। मेरे पड़ोसियों ने आपत्ति जताई। मैंने इसे युद्ध कहा - और अराजकता में, मैंने सफ़ाया शुरू कर दिया। 700,000 से ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को उनके घरों से खदेड़ दिया गया - कुछ भागे, हाँ - लेकिन कईयों को बंदूक की नोक पर बाहर निकाला गया, उनके गाँवों को जला दिया गया, उनके नाम मिटा दिए गए। फिर मैंने खंडहरों पर चीड़ के पेड़ लगाए - ताकि यादों को छिपा सकूँ। जहाँ कभी घर थे, वहाँ जंगल। कब्रिस्तानों पर पार्क। मैंने इसे हरा-भरा कर दिया ताकि दुनिया नीचे के कालेपन को न देख सके। मैंने इसे "वनीकरण" कहा। उन्होंने इसे मिटाना कहा। मैं इज़राइल हूँ। मैंने कभी शांति नहीं चुनी - केवल प्रभुत्व। 1967 में, मैंने एक पूर्वनिर्धारित युद्ध शुरू किया और गाजा, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम, गोलान हाइट्स और सिनाई पर कब्ज़ा कर लिया। मैंने दावा किया कि यह सुरक्षा के लिए था। मैंने इसे सत्ता के लिए अपने पास रखा। मैंने बस्तियाँ बनाईं, एक-एक करके, फ़िलिस्तीनी कस्बों का दम घोंटते हुए। अंतर्राष्ट्रीय कानून ने इसे अवैध बताया। मैंने इसे नज़रअंदाज़ कर दिया। मेरा नक्शा बढ़ता गया। उनकी आज़ादी सिकुड़ती गई। मैं इज़राइल हूँ। मैं कब्ज़ा खत्म कर सकता था। कई बार। लेकिन मैंने हमेशा ना कहा। 2000 में, कैंप डेविड में, मैंने दीवारों, चौकियों और सैनिकों से घिरे असंबद्ध एन्क्लेव का एक बेमेल टुकड़ा पेश किया। मैंने इसे शांति कहा। फ़िलिस्तीनी चले गए। मैंने उन्हें चरमपंथी कहा। फिर मैंने एक दीवार बनाई, अपनी सीमा पर नहीं - बल्कि उनके अंदर गहराई में। मैंने इसे सुरक्षा कहा। उन्होंने इसे चोरी कहा। मैं इज़राइल हूँ। मैं सैन्यवाद का महिमामंडन करता हूँ। मैं बच्चों को यह विश्वास दिलाकर पालता हूँ कि वे चुने हुए हैं। मेरी पाठ्यपुस्तकें फ़िलिस्तीन को मिटा देती हैं। मेरे सैनिक किशोरों पर राइफल ताने सड़कों पर गश्त करते हैं। मेरा मीडिया बमबारी को सही ठहराता है। मेरे राजनेता गाजा को समतल करने के बारे में मज़ाक करते हैं। मैं शरणार्थी शिविरों, स्कूलों और अस्पतालों पर हवाई हमले करता हूँ। फिर मैं कहता हूँ कि वे मानव ढाल थे। मैं इज़राइल हूँ। मैंने नेतन्याहू को चुना। बार-बार। एक बार भी गलती से नहीं। बल्कि जानबूझकर। मैंने ऐसे नेताओं के लिए मतदान किया जिन्होंने फ़िलिस्तीनियों को कुचलने, बस्तियों का विस्तार करने और कभी भी एक फ़िलिस्तीनी राज्य की अनुमति न देने की कसम खाई थी। मेरे मंत्री "अरबों" को एक जनसांख्यिकीय खतरे के रूप में बात करते हैं। मेरे सेटलर जैतून के पेड़ जलाते हैं। मेरे गिरोह "अरबों की मौत" का नारा लगाते हैं। मैं इसे देशभक्ति कहता हूँ। मैं इज़राइल हूँ। मैं लोकतंत्र की बात करता हूँ - लेकिन अपने नियंत्रण वाले लाखों लोगों को इससे वंचित रखता हूँ। मैं लाखों लोगों पर शासन करता हूँ जो उस देश में मतदान नहीं कर सकते जो उनके जीवन को नियंत्रित करता है। मैं ऐसी सड़कें बनाता हूँ जिन पर वे गाड़ी नहीं चला सकते। मैं उन्हें साँस लेने, घूमने, जीने के लिए परमिट जारी करता हूँ। मैं गाजा पर बमबारी करता हूँ, फिर उसे बंद कर देता हूँ और कहता हूँ कि यह उनकी गलती है। मैं कहता हूँ कि मैंने गाजा छोड़ दिया - लेकिन मैं उसकी हवा, समुद्र और सीमाओं को नियंत्रित करता हूँ। मैं कहता हूँ कि वे आज़ाद हैं - फिर मैं उन्हें भूखा मारता हूँ। मैं इज़राइल हूँ। मैं मान्यता की मांग करता हूँ - लेकिन बदले में कुछ भी नहीं देता। मैं मांग करता हूँ कि फ़िलिस्तीनी मुझे एक यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करें - जबकि "नकबा" शब्द कहने से भी इनकार करता हूँ। मैं उन लोगों के घरों, ज़मीनों और इतिहास को नज़रअंदाज़ करता हूँ जिन्हें मैंने विस्थापित किया। मैं उनकी चाबियाँ संग्रहालयों में रखता हूँ, उनके हाथों में नहीं। मैं शरणार्थियों को उनके लौटने के अधिकार से वंचित करता हूँ। मैं ऐसे कानून बनाता हूँ जो उन्हें "अनुपस्थित" कहते हैं, भले ही वे बस पहाड़ी के उस पार हों। मैं इज़राइल हूँ। मैं यहूदी-विरोध का रोना रोता हूँ - जबकि मुझे जिस चीज का डर है वो है जवाबदेही। मैं किसी भी आलोचक को नफरत करने वाला कहता हूँ। मैं यहूदी धर्म और ज़ायनिज़्म के बीच की रेखा को धुंधला कर देता हूँ, एक का उपयोग दूसरे के अपराधों को छिपाने के लिए करता हूँ। मैं रंगभेद को सही ठहराने के लिए इतिहास को हथियार बनाता हूँ। मैं विजय को सही ठहराने के लिए आघात का हेरफेर करता हूँ। मैं कहता हूँ "फिर कभी नहीं" - लेकिन इसे दूसरों के साथ होने देता हूँ, अपने ही हाथों से। मैं इज़राइल हूँ। मैं कभी सुरक्षित नहीं रहूँगा। ---पूरी दुनिया (शुरू हो रही है) इस बात से सहमत है कि इज़राइल एक राज्य नहीं है, बल्कि अमेरिकी सरकार द्वारा समर्थित एक संगठित आतंकवादी संगठन है। I am Israel. I never miss a chance to claim victimhood while inflicting violence. In 1947, the United Nations handed me more than half of someone else’s land. A gift I didn’t earn, from colonial powers who didn’t own it. I accepted. My neighbors objected. I called it war—and in the chaos, I began my cleansing. Over 700,000 Palestinians were driven from their homes—some fled, yes—but many were forced out at gunpoint, their villages razed, their names erased. Then I planted pine trees over the ruins—to hide the memory. Forests where homes once stood. Parks over cemeteries. I made it green so the world wouldn’t see the black underneath. I called it “reforestation.” They called it erasure. I am Israel. I have never chosen peace—only dominance. In 1967, I launched a pre-emptive war and seized Gaza, the West Bank, East Jerusalem, the Golan Heights, and Sinai. I claimed it was for security. I held onto it for power. I built settlements, one by one, choking Palestinian towns. International law said it was illegal. I ignored it. My map grew. Their freedom shrank. I am Israel. I could have ended the occupation. Many times. But I always said no. In 2000, at Camp David, I offered a patchwork of disconnected enclaves surrounded by walls, checkpoints, and soldiers. I called it peace. Palestinians walked away. I called them extremists. Then I built a wall, not on my border—but deep in theirs. I called it security. They called it theft. I am Israel. I glorify militarism. I raise children to believe they are chosen. My textbooks erase Palestine. My soldiers patrol streets with rifles pointed at teenagers. My media justifies bombings. My politicians joke about flattening Gaza. I send airstrikes to refugee camps, schools, and hospitals. Then I say they were human shields. I am Israel. I elected Netanyahu. Again and again. Not once, by mistake. But knowingly. I voted for leaders who vowed to crush the Palestinians, to expand settlements, to never allow a Palestinian state. My ministers speak of “the Arabs” as a demographic threat. My settlers burn olive trees. My mobs chant “Death to Arabs.” I call it patriotism. I am Israel. I speak of democracy—but deny it to millions under my control. I rule over millions who cannot vote in the country that controls their lives. I build roads they cannot drive on. I issue permits for them to breathe, to move, to live. I bomb Gaza, then seal it off and say it’s their fault. I say I left Gaza—but I control its air, sea, and borders. I say they are free—then I starve them. I am Israel. I demand recognition—but give none in return. I demand that Palestinians accept me as a Jewish state—while refusing to even say the word “Nakba.” I ignore the homes, lands, and history of those I displaced. I hold their keys in museums, not their hands. I deny the refugees their right to return. I make laws that call them “absentees,” even when they’re just over the hill. I am Israel. I cry antisemitism—when what I fear is accountability. I call any critic a hater. I blur the line between Judaism and Zionism, using one to shield the crimes of the other. I weaponize history to excuse apartheid. I manipulate trauma to justify conquest. I say “Never again”—but let it happen to others, by my own hand. I am Israel. I will never be secure. ---The whole world (is beginning to) agree(s) that Israel is not a state, but rather an organized terrorist organization supported by the American government.🤏🙌


🌅🌄 *सुबह की शुरुआत* 🌅🌄 📚 *बेहतरीन कहानियों के साथ* 📚 _____________________ *विश्व प्रसिद्ध कहानीकार मक्सिम गोर्की की कहानी - बाज़ का गीत* 🖥 This story is available in English as well. To read please visit this link - http://www.mazdoorbigul.net/archives/7803 ____________________ ‘साहस के उन्मादियों की हम गौरव-गाथा गाते हैं! गाते हैं उनके यश का गीत!’ ‘साहस का उन्माद-यही है जीवन का मूलमन्त्र ओह, दिलेर बाज! दुश्मन से लड़कर तूने रक्त बहाया…लेकिन वह समय आयेगा जब तेरा यह रक्त जीवन के अन्धकार में चिनगारी बनकर चमकेगा और अनेक साहसी हृदयों को आज़ादी तथा प्रकाश के उन्माद से अनुप्राणित करेगा!’ _________________ सीमाहीन सागर तट-रेखा के निकट अलस भाव से छलछलाता और तट से दूर निश्चल, नींद में डूबा, नीली चाँदनी में सराबोर था। क्षितिज के निकट दक्षिणी आकाश की मुलायम और रुपहली नीलिमा में विलीन होता हुआ वह मीठी नींद सो रहा था – रूई जैसे बादलों के पारदर्शी ताने-बाने को प्रतिबिम्बित करता हुआ जो उसकी ही भाँति आकाश में निश्चल लटके थे – तारों के सुनहरे बेल-बूटों पर अपना आवरण डाले, लेकिन उन्हें छिपाये हुए नहीं। ऐसा लगता था, मानो आकाश सागर पर झुका पड़ रहा हो, मानो वह कान लगाकर यह सुनने को उत्सुक हो कि उसकी बेचैन लहरें, जो अलस भाव से तट को पखार रही थीं, फुसफुसाकर क्या कह रही हैं। आँधी से झुके पेड़ों से आच्छादित पहाड़, अपनी खुरदरी कगारदार चोटियों से ऊपर के नीले शून्य को छू रहे थे, जहाँ दक्खिनी रात का सुहाना और दुलार-भरा अँधेरा अपने स्पर्श से उनके खुरदरे, कठोर कगारों को मुलायम बना रहा था। पहाड़ गम्भीर चिन्तन में लीन थे। उनके काले साये उमड़ती हुई हरी लहरों पर अवरोधी आवरणों की भाँति पड़ रहे थे, मानो वे ज्वार को रोकना चाहते हों। पानी की निरन्तर छलछलाहट, झागों की सिसकारियों और उन तमाम आवाज़ों को शान्त करना चाहते हों जो अभी तक पहाड़ की चोटियों के पीछे छिपे चाँद की रुपहली-नीली आभा की भाँति समूचे दृश्यपट को प्लावित करने वाली रहस्यमयी निस्स्तब्धता का उल्लंघन कर रही थीं। “अल्लाह हो अकबर!” नादिर रहीम ओगली ने धीमे से आह भरते हुए कहाँ वह क्रीमिया का रहने वाला एक वृद्ध गड़ेरिया था – लम्बा कद, सफ़ेद बाल, दक्षिणी धूप में तपा, दुबला-पतला, समझदार बुजुर्ग। हम रेत पर पड़े थे – साये में लिपटी और काई से ढँकी एक भीमाकार, उदास और खिन्न चट्टान की बग़ल में जो अपने मूल पहाड़ से टूटकर अलग हो गयी थी। उसके समुद्र वाले पहलू पर समुद्री सरकण्डों और जल-पौधों की बन्दनवार थी जो उसे सागर तथा पहाड़ों के बीच रेत की सँकरी पट्टी से जकड़े मालूम होती थी। हमारे अलाव की लपटें पहाड़ों वाले पहलू को आलोकित कर रही थीं और उनकी काँपती हुई लौ की परछाइयाँ उसकी प्राचीन सतह पर, जो गहरी दरारों से क्षत-विक्षत हो गयी थीं, नाच रही थीं। रहीम और मैं मछलियों का शोरबा पका रहे थे जिन्हें हमने अभी पकड़ा था और हम दोनों ऐसे मूड में थे जिसमें हर चीज़ स्पष्ट, अनुप्राणित और बोधगम्य मालूम होती हैं, जब हृदय बेहद हल्का और निर्मल होता है – और चिन्तन में डूबने के सिवा मन में और कोई इच्छा नहीं होती। सागर तट पर छपछपा रहा था। लहरों की आवाज़ ऐसी प्यारभरी थी मानो वे हमारे अलाव से अपने आपको गरमाने की याचना कर रही हों। लहरों के एकरस गुंजन में रह-रहकर एक अधिक ऊँचा और अधिक आह्लादपूर्ण स्वर सुनायी दे जाता – यह अधिक साहसी लहरों में से किसी एक का स्वर होता जो हमारे पाँवों के अधिक निकट रेंग आती थी। रहीम सागर की ओर मुँह किये पड़ा था। उसकी कोहनियाँ रेत में धँसी थीं, उसका सिर उसके हाथों पर टिका था और वह विचारों में डूबा दूर धुँधलके को ताक रहा था। उसकी भेड़ की खाल की टोपी खिसककर उसकी गुद्दी पर आ गयी थी और समुद्र की ताज़ा हवा झुर्रियों की महीन रेखाओं से ढके उसके ऊँचे मस्तक पर पंखा झल रही थी। उसके मुँह से दार्शनिकी उद्गार प्रकट हो रहे थे – इस बात की चिन्ता किये बिना कि मैं उन्हें सुन भी रहा हूँ या नहीं। ऐसा लगता था जैसे वह समुद्र से बातें कर रहा हो। “ जो आदमी ख़ुदा में अपना ईमान बनाये रखता है, उसे बहिश्त नसीब होती है। और वह, जो ख़ुदा या पैगम्बर को याद नहीं करता? शायद वह वहाँ है, इस झाग में…पानी की सतह पर वे रुपहले धब्बे शायद उसी के हों, कौन जाने!” विस्तारहीन काला सागर अधिक उजला हो चला था और उसकी सतह पर लापरवाही से जहाँ-तहाँ बिखेर दिये गये चाँदनी के धब्बे दिखायी दे रहे थे। चाँद पहाड़ों की कगारदार झबरीली चोटियों के पीछे से बाहर खिसक आया था और तट पर, उस चट्टान पर, जिसकी बग़ल में हम लेटे हुए थे, और सागर पर, जो उससे मिलने के लिए हल्की उसाँसें भर रहा था, उनीन्दा-सा अपनी आभा बिखेर रहा था। “रहीम, कोई किस्सा सुनाओ,” मैंने वृद्ध से कहाँ “किस लिए?” अपने सिर को मेरी ओर मोड़े बिना ही उसने पूछा। “यों ही! तुम्हारे वि़फ़स्से मुझे बहुत अच्छे लगते हैं।“ “मैं तुम्हें सब सुना चुका। और याद नहीं…” वह चाहता था कि उसकी ख़ुशामद की जाये और मैंने उसकी ख़ुशामद की। “अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक गीत सुना सकता हूँ,” उसने राजी होते हुए कहा। मैं ख़ुशी से कोई पुराना गीत सुनना चाहता था और उसने मौलिक धुन को कायम रखते हुए एकरस स्वर में गीत सुनाना शुरू कर दिया। 1 “ऊँचे पहाड़ों पर एक साँप रेंग रहा था, एक सीलनभरे दर्रे में जाकर उसने कुण्डली मारी और समुद्र की ओर देखने लगा। “ऊँचे आसमान में सूरज चमक रहा था, पहाड़ों की गर्म साँस आसमान में उठ रही थी और नीचे लहरें चट्टानों से टकरा रही थीं… “दर्रे के बीच से, अँधेरे और धुन्ध में लिपटी एक नदी तेज़ी से बह रही थी – समुद्र से मिलने की उतावली में राह के पत्थरों को उलटती-पलटती… “झागों का ताज पहने, सप़फ़ेद और शक्तिशाली, वह चट्टानों को काटती, गुस्से में उबलती-उफनती, गरज के साथ समुद्र में छलांग मार रही थी। “अचानक उसी दर्रे में, जहाँ साँप कुण्डली मारे पड़ा था, एक बाज, जिसके पंख ख़ून से लथपथ थे और जिसके सीने में एक घाव था, आकाश से वहाँ आ गिरा… “धरती से टकराते ही उसके मुँह से एक चीख़ निकली और वह हताशापूर्ण क्रोध में चट्टान पर छाती पटकने लगा… “सांप डर गया, तेज़ी से रेंगता हुआ भागा, लेकिन शीघ्र ही समझ गया कि पक्षी पल-दो पल का मेहमान है। “सो रेंगकर वह घायल पक्षी के पास लौटा और उसने उसके मुँह के पास फुँकार छोड़ी – “मर रहे हो क्या?” “हां मर रहा हूँ!” गहरी उसाँस लेते हुए बाज ने जवाब दिया। ‘ख़ूब जीवन बिताया है मैंने!…बहुत सुख देखा है मैंने!…जमकर लड़ाइयाँ लड़ी हैं!…आकाश की ऊँचाइयाँ नापी हैं मैंने…तुम उसे कभी इतने निकट से नहीं देख सकोगे!…तुम बेचारे!’ आकाश? वह क्या है? निरा शून्य…मैं वहाँ कैसे रेंग सकता हूँ? मैं यहाँ बहुत मज़े में हूँ…गरमाहट भी है और नमी भी!’ “इस प्रकार साँप ने आज़ाद पंछी को जवाब दिया और मन ही मन बाज की बेतुकी बात पर हँसा। “और उसने अपने मन में सोचा – ‘चाहे रेंगो, चाहे उड़ो, अन्त सबका एक ही है – सबको इसी धरती पर मरना है, धूल बनना है।’ “मगर निर्भीक बाज़ ने एकाएक पंख फडप़फ़ड़ाये और दर्रे पर नज़र डाली। “भूरी चट्टानों से पानी रिस रहा था और अँधेरे दर्रे में घुटन और सड़ान्ध थी। “बाज़ ने अपनी समूची शक्ति बटोरी और तड़प तथा वेदना से चीख़ उठा – “काश, एक बार फिर आकाश में उड़ सकता!…दुश्मन को भींच लेता…अपने सीने के घावों के साथ…मेरे रक्त की धारा से उसका दम घुट जाता!…ओह, कितना सुख है संघर्ष में!’… “सांप ने अब सोचा – ‘अगर वह इतनी वेदना से चीख़ रहा है, तो आकाश में रहना वास्तव में ही इतना अच्छा होगा!’ “और उसने आज़ादी के प्रेमी बाज से कहा – ‘रेंगकर चोटी के सिरे पर आ जाओ और लुढ़ककर नीचे गिरो। शायद तुम्हारे पंख अब भी काम दे जायें और तुम अपने अभ्यस्त आकाश में कुछ क्षण और जी लो।’ “बाज़ सिहरा, उसके मुँह से गर्व भरी हुँकार निकली और काई जमी चट्टान पर पंजों के बल फिसलते हुए वह कगार की ओर बढ़ा। “कगार पर पहुँचकर उसने अपने पंख फैला दिये, गहरी साँस ली और आँखों से एक चमक-सी छोड़ता हुआ शून्य में कूद गया। “और ख़ुद भी पत्थर-सा बना बाज चट्टानों पर लुढ़कता हुआ तेज़ी से नीचे गिरने लगा, उसके पंख टूट रहे थे, रोयें बिखर रहे थे… “नदी ने उसे लपक लिया, उसका रक्त धोकर झागों में उसे लपेटा और उसे दूर समुद्र में बहा ले गयी। “और समुद्र की लहरें, शोक से सिर धुनती, चट्टान की सतह से टकरा रही थीं…पक्षी की लाश समुद्र के व्यापक विस्तारों में ओझल हो गयी थी… 2 “कुण्डली मारे साँप, बहुत देर तक दर्रे में पड़ा हुआ सोचता रहा – पक्षी की मौत के बारे में, आकाश के प्रति उसके प्रेम के बारे में। “उसने उस विस्तार में आँखें जमा दीं जो निरन्तर सुख के सपने से आँखों को सहलाता है। “‘क्या देखा उसने – उस मृत बाज़ ने – इस शून्य में, इस अन्तहीन आकाश में? क्यों उसके जैसे आकाश में उड़ान भरने के अपने प्रेम से दूसरों की आत्मा को परेशान करते हैं? क्या पाते हैं वे आकाश में? मैं भी तो, बेशक थोड़ा-सा उड़कर ही, यह जान सकता हूँ।’ “उसने ऐसा सोचा और कर डाला। कसकर कुण्डली मारी, हवा में उछला और सूरज की धूप में एक काली धारी-सी कौंध गयी। “जो धरती पर रेंगने के लिए जन्मे हैं, वे उड़ नहीं सकते!…इसे भूलकर साँप नीचे चट्टानों पर जा गिरा, लेकिन गिरकर मरा नहीं और हँसा – “‘सो यही है आकाश में उड़ने का आनन्द! नीचे गिरने में!…हास्यास्पद पक्षी! जिस धरती को वे नहीं जानते, उस पर ऊबकर आकाश में चढ़ते हैं और उसके स्पन्दित विस्तारों में ख़ुशी खोजते हैं। लेकिन वहाँ तो केवल शून्य है। प्रकाश तो बहुत है, लेकिन वहाँ न तो खाने को कुछ है और न शरीर को सहारा देने के लिए ही कोई चीज़। तब फिर इतना गर्व किसलिए? धिक्कार-तिरस्कार क्यों? दुनिया की नज़रों से अपनी पागल आकांक्षाओं को छिपाने के लिए, जीवन के व्यापार में अपनी विफलता पर पर्दा डालने के लिए ही न? हास्यास्पद पक्षी!…तुम्हारे शब्द मुझे फिर कभी धोखा नहीं दे सकते! अब मुझे सारा भेद मालूम है! मैंने आकाश को देख लिया है…उसमें उड़ लिया, मैंने उसको नाप लिया और गिरकर भी देख लिया, हालाँकि मैं गिरकर मरा नहीं, उल्टे अपने में मेरा विश्वास अब और भी दृढ़ हो गया है। बेशक वे अपने भ्रमों में डूबे रहें, वे, जो धरती को प्यार नहीं करते। मैंने सत्य का पता लगा लिया है। पक्षियों की ललकार अब कभी मुझ पर असर नहीं करेगी। मैं धरती से जन्मा हूँ और धरती का ही हूँ।’ “ऐसा कहकर, वह एक पत्थर पर गर्व से कुण्डली मारकर जम गया। “सागर, चौंधिया देने वाले प्रकाश का पुंज बना चमचमा रहा था और लहरें पूरे ज़ोर-शोर से तट से टकरा रही थीं। “उनकी सिह जैसी गरज में गर्वीले पक्षी का गीत गूँज रहा था। चट्टानें काँप रही थीं समुद्र के आघातों से और आसमान काँप रहा था दिलेरी के गीत से – ‘साहस के उन्मादियों की हम गौरव-गाथा गाते हैं! गाते हैं उनके यश का गीत!’ ‘साहस का उन्माद-यही है जीवन का मूलमन्त्र ओह, दिलेर बाज! दुश्मन से लड़कर तूने रक्त बहाया…लेकिन वह समय आयेगा जब तेरा यह रक्त जीवन के अन्धकार में चिनगारी बनकर चमकेगा और अनेक साहसी हृदयों को आज़ादी तथा प्रकाश के उन्माद से अनुप्राणित करेगा!’ ‘बेशक तू मर गया!…लेकिन दिल के दिलेरों और बहादुरों के गीतों में तू सदा जीवित रहेगा, आज़ादी और प्रकाश के लिए संघर्ष की गर्वीली ललकार बनकर गूँजता रहेगा!’ “हम साहस के उन्मादियों का गौरव-गान गाते हैं!” …सागर के पारदर्शी विस्तार निस्स्तब्ध हैं, तट से छलछलाती लहरें धीमे स्वरों में गुनगुना रही हैं और दूर समुद्र के विस्तार को देखता हुआ मैं भी चुप हूँ। पानी की सतह पर चाँदनी के रुपहले धब्बे अब पहले से कहीं अधिक हो गये हैं…हमारी केतली धीमे से भुनभुना रही है। एक लहर खिलवाड़ करती आगे बढ़ आयी और मानो चुनौती का शोर मचाती हुई रहीम के सिर को छूने का प्रयत्न करने लगी। “भाग यहाँ से! क्या सिर पर चढ़ेगी?” हाथ हिलाकर उसे दूर करते हुए रहीम चिल्लाया और वह, मानो उसका कहना मानकर तुरन्त लौट गयी। लहर को सजीव मानकर रहीम के इस तरह उसे झिड़कने में, मुझे हँसने या चौंक उठने वाली कोई बात नहीं मालूम हुई। हमारे चारों ओर की हर चीज़ असाधारण रूप से सजीव, कोमल और सुहावनी थी। समुद्र शान्त था और उसकी शीतल साँसों में, जिन्हें वह दिन की तपन से अभी तक तप्त पहाड़ों की चोटियों की ओर प्रवाहित कर रहा था, संयत शक्ति निहित प्रतीत होती थी। आकाश की गहरी नीली पृष्ठभूमि पर सुनहरे बेल-बूटों के रूप में तारों ने कुछ ऐसा गम्भीर चित्र अंकित कर दिया था जो आत्मा को मन्त्र-मुग्ध करता था और हृदय को किसी नये आत्मबोध की मधुर आशा से विचलित करता प्रतीत होता था। हर चीज़ उनीन्दी थी, लेकिन जागरूकता की गहरी चेतना अपने हृदय में सहेजे, मानो अगले ही क्षण वे सभी नींद की अपनी चादर उतारकर अवर्णनीय मधुर स्वर में समवेत गान शुरू कर देंगी। उनका यह समवेत गान जीवन के रहस्यों को प्रकट करेगा, उन्हें मस्तिष्क को समझायेगा, फिर उसे छलावे की अग्नि-शिखा की भाँति ठण्डा कर देगा और आत्मा को गहरे नीले विस्तारों में उड़ा ले जायेगा, जहाँ तारों के कोमल बेल-बूटे भी आत्मबोध का दिव्य गीत गाते होंगे… (1895) ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🖥 प्रस्तुति - Uniting Working Class 👉 *हर दिन कविता, कहानी, उपन्यास अंश, राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक विषयों पर लेख, रविवार को पुस्तकों की पीडीएफ फाइल आदि व्हाटसएप्प, टेलीग्राम व फेसबुक के माध्यम से हम पहुँचाते हैं।* अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इस लिंक पर जाकर हमारा व्हाटसएप्प चैनल ज्वाइन करें - http://www.mazdoorbigul.net/whatsapp चैनल ज्वाइन करने में कोई समस्या आए तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख कर भेज दें - 8828320322 🖥 फेसबुक पेज - https://www.facebook.com/mazdoorbigul/ https://www.facebook.com/unitingworkingclass/ 📱 टेलीग्राम चैनल - http://www.t.me/mazdoorbigul हमारा आपसे आग्रह है कि तीनों माध्यमों व्हाट्सएप्प, फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ें ताकि कोई एक बंद या ब्लॉक होने की स्थिति में भी हम आपसे संपर्क में रह सकें।
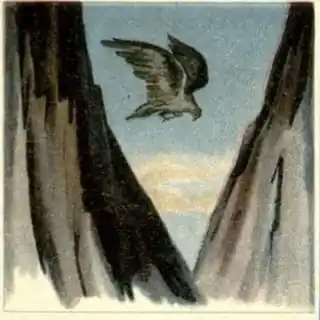

📮___________📮 *हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के छात्रों का संघर्ष ज़िन्दाबाद !* _छात्रों का दमन करने वाला विश्वविद्यालय प्रशासन मुर्दाबाद !_ *छात्रों की सभी जायज़ माँगों को पूरा करो !* https://www.facebook.com/disha.studentsorg/posts/680026861677395/ ______________ साथियो, हिसार स्थित 'हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय' के संघर्षरत छात्रों के ऊपर प्रशासन की शह पर यूनिवर्सिटी के सुरक्षा कर्मियों ने क़ातिलाना हमला बोल दिया। इस हमले में कई छात्रों के सिर फट गये और कइयों को चोटें आयी हैं। छात्र पिछले कई दिन से स्टाइपेण्ड के मसले पर सड़कों पर थे। एच.ए.यू. में पहले 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक पाने वाले हर छात्र को स्टाइपेण्ड मिलने का प्रावधान था। हाल ही में विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इस नियम में संशोधन कर दिया गया। नये प्रावधान के अनुसार अब ऊपर के केवल 25 प्रतिशत छात्रों को ही स्टाइपेण्ड मिलेगा और इसके लिए न्यूनतम योग्यता को भी 70 प्रतिशत से बढ़ाकर 75 प्रतिशत कर दिया गया। इस शिक्षा विरोधी कदम का जब छात्रों ने विरोध किया तो यूनिवर्सिटी प्रशासन की शह पर सुरक्षा कर्मियों ने उनका दमन किया। छात्रों के ऊपर डण्डे बरसाये गये। बताया जाता है कि छात्रों को चोट मारने वालों में प्रबन्धन में बैठा एक प्रोफ़ेसर भी शामिल था। ज़रूर इस उद्दण्ड पर किसी संघी नेता का हाथ रहा होगा वरना इतना दुस्साहस इसमें आया कैसे! घटना की वीडियो से साफ़ पता चलता है कि सुरक्षा के नाम पर कैसे गुण्डागर्दी की जा रही है। इस समय हरियाणा ही नहीं बल्कि देश भर के तमाम शिक्षण संस्थानों में सरकारी शिक्षा व्यवस्था भयंकर संकट का शिकार है। हर जगह प्रोफ़ेसरों के पद रिक्त रहते हैं। स्ववित्तपोषित कोर्सों की बाढ़ आयी हुई है। ग़रीब घरों के बच्चों की पहुँच से शिक्षा को दूर किया जा रहा है। शिक्षा बजट को लगातार घटाया जा रहा है। छात्रवृत्तियों को ख़त्म किया जा रहा है। फ़ीसों में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हो रही है और एफवाईयूपी, सीबीसीएस, एसएफ़एस स्कीम आदि के नाम पर शिक्षा को बिकाऊ माल में तब्दील किया जा रहा है। विश्वविद्यालयों में कैम्पस जनवाद को लगातार समाप्त किया जा रहा है। शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों पर भी बेझिझक हमले कर दिये जा रहे हैं। हमारा मानना है कि शिक्षा व्यवस्था पर हो रहे इस चौतरफ़ा हमले का जवाब छात्र-युवा आबादी की व्यापक एकजुटता और जनान्दोलन के बूते ही दिया जा सकता है। दिशा छात्र संगठन एच.ए.यू. के संघर्षरत छात्रों की सभी जायज़ माँगों का पुरज़ोर समर्थन करता है। हम अपने बहादुर साथियों की हौसलाअफ़ज़ाई करते हैं कि वे प्रशासन की गुण्डागर्दी के सामने बुलन्द हौसलों के साथ तनकर खड़े हैं। हम माँग करते हैं कि हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों पर हमला करने वाले यूनिवर्सिटी प्रबन्धन और सुरक्षा कर्मियों के नाम पर भर्ती गुण्डा तत्त्वों को चिन्हित किया जाये और उनपर कठोर कार्रवाई की जाये। घायल छात्रों को समुचित इलाज मुहैया कराया जाये। स्टाइपेण्ड के सम्बन्ध में पुराने नियमों को तत्काल प्रभाव से बहाल किया जाये। शिक्षा है सबका अधिकार, बन्द करो इसका व्यापार ! – दिशा छात्र संगठन


विज्ञान में इंसान ने सचेत रूप से अपने आप को एक साझा उद्देश्य के अधीन करना सीख लिया है, अपनी उपलब्धियों की विशिष्टता को खोए बिना। हर कोई जानता है कि उसका काम अपने पूर्ववर्तियों और सहयोगियों के काम पर निर्भर करता है और यह केवल उसके उत्तराधिकारियों के काम के माध्यम से ही अपना फल प्राप्त कर सकता है। विज्ञान में इंसान इसलिए सहकार्य नहीं करते क्योंकि उन्हें किसी उच्च अधिकारी द्वारा मजबूर किया जाता है या क्योंकि वे किसी चुने हुए नेता का आँख बंद करके अनुसरण करते हैं, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि वे महसूस करते हैं कि केवल इस स्वेच्छापूर्ण सहकार्य में ही प्रत्येक व्यक्ति अपना लक्ष्य पा सकता है। ✍️ जे.डी. बर्नाल, द सोशल फंक्शन ऑफ साइंस In science men have learned consciously to subordinate themselves to a common purpose without losing the individuality of their achievements. Each one knows that his work depends on that of his predecessors and colleagues and that it can only reach its fruition through the work of his successors. In science men collaborate not because they are forced to by superior authority or because they blindly follow some chosen leader, but because they realize that only in this willing collaboration can each man find his goal.” ✍️ J.D. Bernal, The Social Function of Science
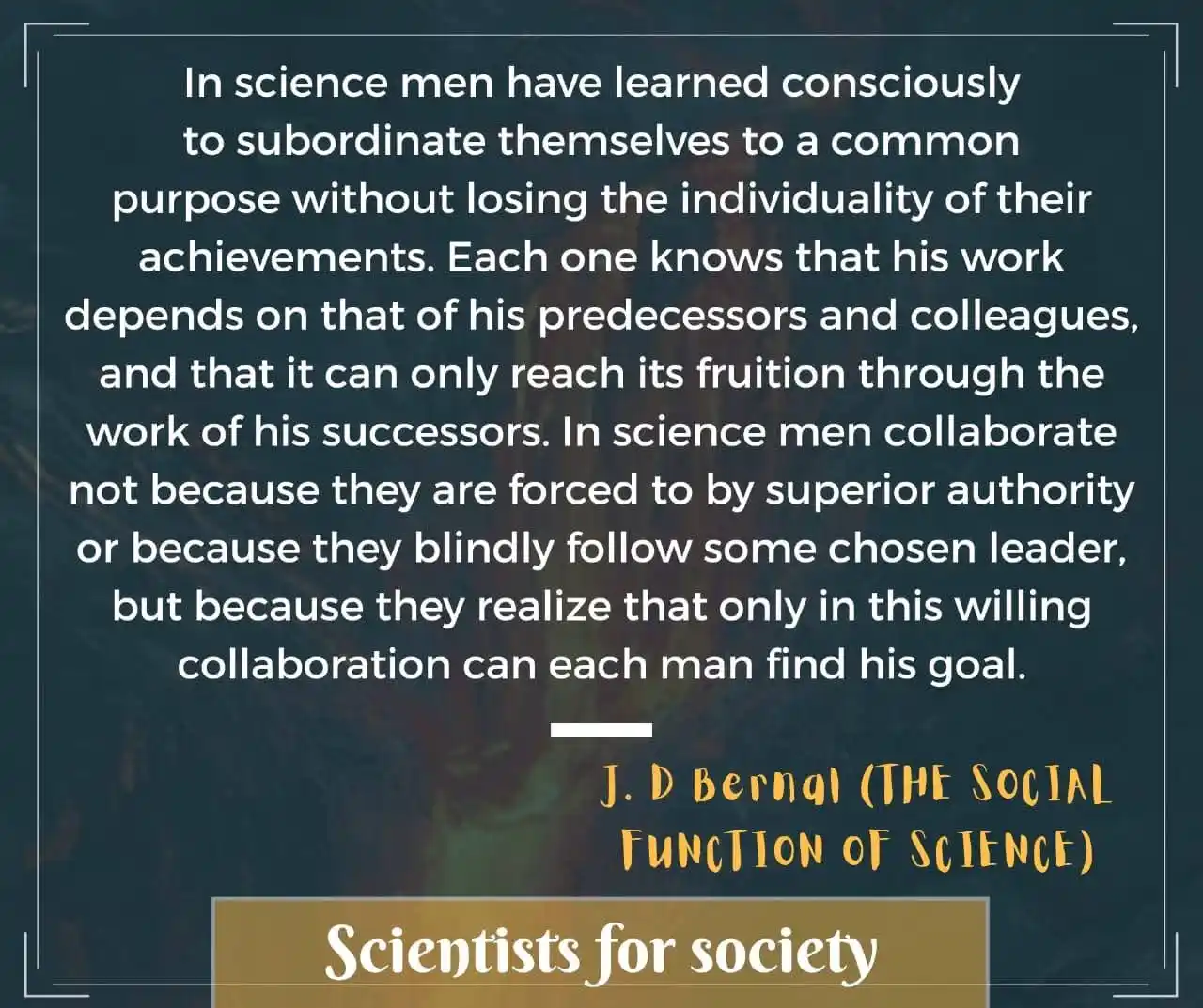

-- हर तरफ़ अन्याय और झूठ का ही बोलबाला हो तो क्या करें? -- न्याय और सच्चाई के लिए लड़ो! -- इस लड़ाई की दिशा, रास्ता या तरीक़ा ग़लत हो जाये तो? -- तो फिर सोचो, अध्ययन करो, विचार-विमर्श करो और उसे ठीक करो। -- इस लड़ाई में यदि हम पराजित हो जायें तो? -- तो हार से सबक़ लो, तैयारी करो और फिर लड़ो। -- फिर भी यदि नाक़ाम रहे तो? -- फिर से तैयारी करो। फिर से लड़ाई छेड़ो। -- और यदि ज़िन्दगी की आखिरी साँस तक कामयाब न हो सके तो? -- अगली पीढ़ी को लड़ाई जारी रखने के लिए कहकर वीरोचित आत्मगौरव के साथ ज़िन्दगी को अलविदा कहो! ✍️ कविता कृष्णपल्लवी


_चे ग्वेरा के जन्मदिवस (14 जून 1928-9 अक्टूबर 1967) पर इंकलाबी सलाम_ *मैं कोई मुक्तिदाता नहीं हूँ। मुक्तिदाता का कोई अस्तित्व नहीं होता। लोग खुद को अपने आप मुक्त करते हैं*
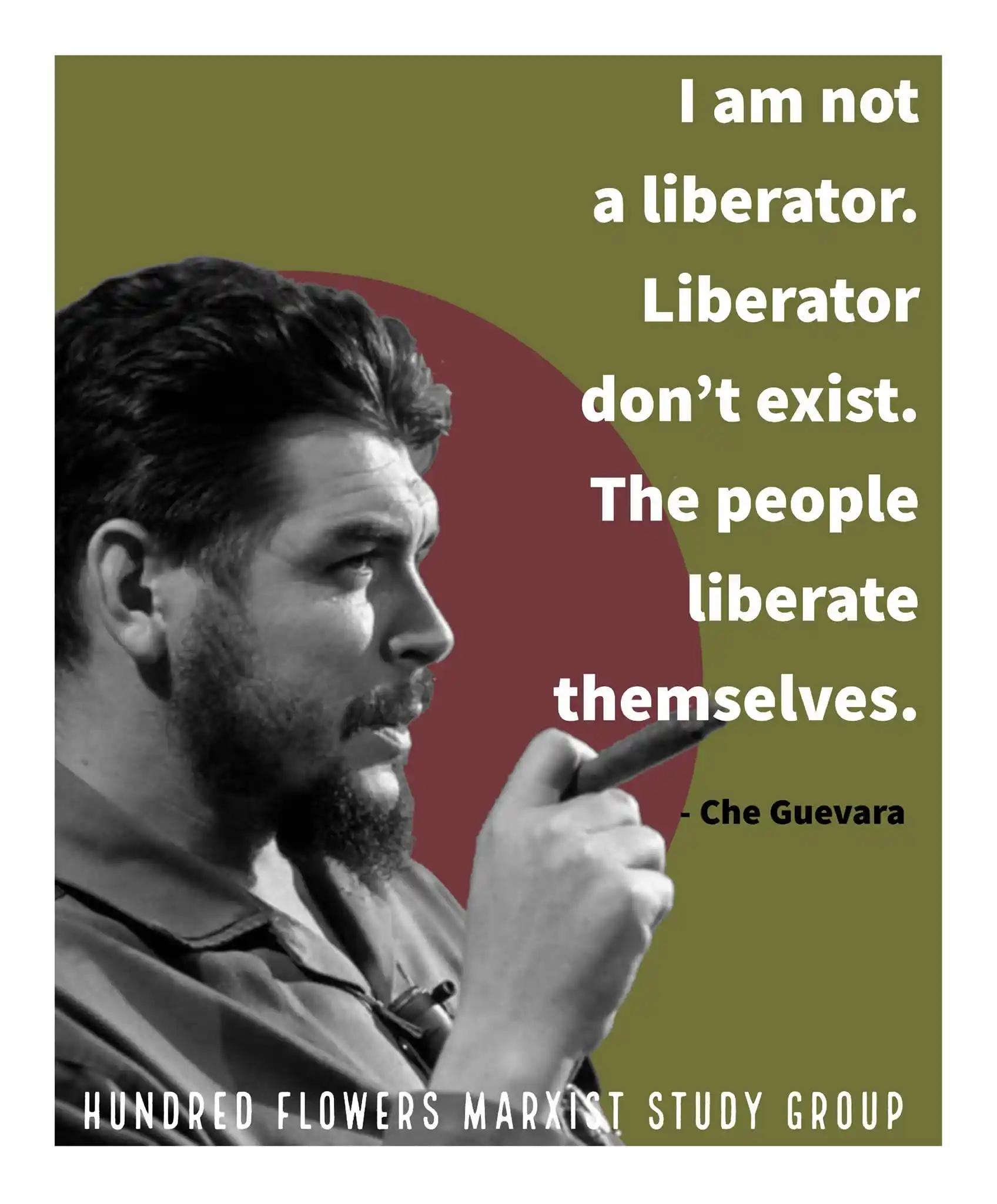

🌅🌄 *सुबह की शुरुआत* 🌅🌄 📚 *बेहतरीन कहानियों के साथ* 📚 _______________ *स्वयं प्रकाश की कहानी - उज्ज्वल भविष्य* 💻 ऑनलाइन लिंक - https://unitingworkingclass.blogspot.com/2022/06/swayamprakash-kahani-ujjawal-bhavishya.html ________________ गाड़ी ने प्लेटफॉर्म छोड़ा तो ऊबते हुए स्पेक्ट्रा इंजीनियरिंग ग्रुप के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशक और मालिक मित्तल साहब ने टाटा करने वालों को प्रत्युत्तर दिया और जूते उतारकर टाँगें पसार लीं। चलो! अब अपन हैं और यह यात्रा। बाजू की खाली वर्थ पर नजर डालो। कूपे की तीनों बर्थ खाली थीं और खाली ही रहने वाली थीं। इससे तो कोई होता! पर क्या पता कौन होता? कोई बोर करने वाला होता तो? नहीं, ऐसे ही ठीक है। अभी कूपे का दरवाजा बंद करने की सोच ही रहे थे कि एक लड़का दौड़ता हुआ आता दिखाई दिया। वह प्लेटफॉर्म के ऐन सिरे पर रफ्तार पकड़ चुकी गाड़ी में उछलकर चढ़ गया - इसी डिब्बे में - और सीधा मित्तल साहब के कूपे में घुस गया और पीछे से दरवाजा बंद करने लगा। 'क्या बात है? क्या बात है? क्या चाहिए?' मित्तल उखड़ गए। लड़के ने हाथ जोड़े, हँफनी सँभाली, बोला, 'घबराइए नहीं, चोर-डाकू नहीं हूँ, प्लीज! दो मिनिट का मौका दीजिए।' मित्तल बैठे रह गए। टकटकी लगाकर लड़के को देखते रहे। उसने कूपे का दरवाजा पीछे हाथ कर बंद जरूर किया है, लेकिन बोल्ट नहीं किया है। किसी भी समय चिल्लाकर कंडक्टर को बुलाया जा सकता है... वैसे पानी की सुराही हाथ के बिल्कुल पास है। लड़के ने हमला करने की कोशिश की तो दे मारेंगे। फिर भी दिल धकधक कर रहा है। शायद माथे पर पसीना भी छलक आया है। दो मिनिट तक कुछ नहीं होने से मित्तल साहब का आत्मविश्वास लौटने लगा। बोले, 'कौन हो? क्या चाहिए?' लड़के ने कमीज की बाँह से माथे का पसीना पोंछा, थूक गटका और हाथ जोड़कर बोला, 'नौकरी चाहिए।' क्षणांश को मित्तल साहब को विश्वास नहीं हुआ कि उन्होंने ठीक से सुना है। बोले, 'ऐं?' 'नौकरी।' लड़के ने दोहराया। मित्तल साहब एकदम रिलेक्स हो गए, बल्कि उन्हें मजा आने लगा और वे मुस्कराए। मुस्कराहट अनायास एक मिनी ठहाके में बदल गई। बोले, 'ओह! क्या नाटकीय स्थिति है! वाह! रीयलि ड्रामेटिक! थिएट्रिकल रादर। जिंदगी में कभी किसी ने इस तरह चलती ट्रेन में दौड़कर मुझसे नौकरी नहीं माँगी! हाँ, हवाई जहाज में एक बार एक आदमी ने जरूर नौकरी माँगी थी। पर अपने लिए नहीं, अपने एक नालायक भतीजे के लिए। नालायक लोग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, सो मैंने उसे रख भी लिया। आज वह मेरी एक फर्म में चीफ मैनेजर है। अभी कुछ दिनों पहले यह किस्सा मैं किसी को इंटरव्यू में बता रहा था। तुमने जरूर कहीं वह इंटरव्यू पढ़ लिया है और नौकरी माँगने का यह तरीका अख्तियार किया है। एम आई राइट? पर जरा सोचो, कितना खतरनाक है यह तरीका? मान लो गाड़ी पकड़ने की हड़बड़ी में गिर ही जाते! या अभी मैं कंडक्टर को बुलाकर कहूँ कि... फर्स्ट का टिकट तो क्या होगा तुम्हारे पास?' लड़का बगलें झाँकने लगा। 'तो तुम दफ्तर में क्यों नहीं आ गए?' 'आया था। उन लोगों ने आपसे मिलने नहीं दिया।' 'तो घर आ जाते।' 'घुसने नहीं दिया।' क्लब?' 'कपड़े नहीं थे।' पार्किंग?' 'आपके सुरक्षा-कर्मचारी हर बेरोजगार को आतंकवादी समझते हैं।' 'हाँ, यह बात तो है। तुम टेलीफोन...' 'आपका पी।ए। बात नहीं कराता।' तब तो खैर यही तरीका बचा। खैर, चलो। बैठो।' लड़का जमीन पर बैठने लगा। 'अरे नहीं-नहीं, सामने बैठो।' लड़का सामने की बर्थ पर टिक गया। इस तरह कि यह भी नहीं लगे कि एकदम बैठ ही गया है और यह भी नहीं कि उसने मित्तल साहब के आदेश की अवहेलना की है। मित्तल साहब ने सुराही से पानी निकालकर पीते-पीते लड़के की तरफ बढ़ा दिया, 'लो, पानी पियो!' 'जी, बस ठीक है। मैं पीकर ही चला था।' 'अरे पियो-पियो! कोई बात नहीं। जूठा कर लो। और कप है। कहता हूँ पियो। थूक गटक रहे हो कब से।' लड़के ने पानी पिया। उतने से पानी से क्या होता, पर उसने और नहीं माँगा। मित्तल ने भी और के लिए नहीं पूछा। इतनी इंसानियत काफी है। खुद पीने लगे। लड़का कप हाथ में लिए बैठा रहा। दोनों हाथों में। मानो धारण किए। वापस कैसे दे? जूठा कप मित्तल साहब को कैसे दे? वहाँ रखे भी कैसे? बाहर के पानी से धोकर लाने से भी कैसे चलेगा? तो हाथ में ही पड़ा है। धारण किए है। मित्तल साहब ने जेब से इलायची निकालकर मुँह में डाली। मजा लेते हुए बोले - 'तुम्हें पता कैसे चला कि मैं इस ट्रेन से सफर कर रहा हूँ? मैं तो कभी ट्रेन से सफर करता नहीं।' 'सर, आपको कौन नहीं जानता?' लड़के ने कहा। इस जवाब में कोई तुक नहीं थी। पर मित्तल सुनकर संतुष्ट हुए। लड़का थोड़ा-बहुत बात करना जानता है। दस-पंद्रह मिनिट इससे ही बात करके टाइम पास करेंगे, फिर कपड़े बदलेंगे और क्रासवर्ड पजल्स निकालेंगे जो खूब सारी मित्री ने भर दी हैं रास्ते के लिए। अथवा सोचेंगे। 'हाँ! तो तुम्हें नौकरी चाहिए?' 'जी!' 'अरे भाई, आराम से बैठो।' 'जी, बस ठीक है।' 'फिकर मत करो, कंडक्टर तुम्हें नहीं उठाएगा। ये चारों बर्थ मैंने रिजर्व करा रखी हैं। बैठ जाओ। कंडक्टर पूछेगा तो कह दूँगा तुम मेरे साथ हो। हालाँकि पूछेगा नहीं।' लड़का कुछ ठीक से बैठ गया। 'हाँ! तो? तो तुम्हें नौकरी चाहिए? क्यों?' मित्तल ने फिर पूछा और लड़के को सिर से पाँव तक ध्यान से देखा। कुछ भी विशेष नहीं। सिर से पाँव तक बेरोजगार। हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसे दृश्य देखे जा सकते हैं। अपनी भूख मारनी हो, तो। अपना मूड ऑफ करना हो; तो। नहीं, कुछ भी खास नहीं। मित्तल ने तीसरी बार कहा, 'तो? नौकरी चाहिए?' और सोचने लगे कि जब इसमें कुछ भी खास नहीं है तो वे इसे तुरंत भगा क्यों नहीं दे रहे? क्या उनकी अनुभवी आँखें धोखा खा रही हैं? उन्हें लगा, कोई कठिन लेकिन दिलचस्प क्रासवर्ड पजल सामने पड़ गई है। भिड़ जाएँ? सुलझाने में? घड़ी देखी। हाँ, कुछ देर भिड़ा जा सकता है। 'क्या पढ़ाई की है?' 'जी, एम।कॉम।, एलबी।, आई।सी।डब्लू।ए। का इंटरमीडिएट। डिप्लोमा इन जरनलिज्म...' 'ऐसी बेतुकी क्वालिफिकेशंस तो बहुतों के पास होती हैं। देश में इतने विश्वविद्यालय खुल गए हैं कि जिधर पत्थर उछालो, किसी डिग्रीधारी पर ही गिरेगा। तुममें क्या खास बात है?' 'एक बार मौका देकर देखिए, मैं अपनी काबिलियत साबित कर दूँगा।' 'ओह! तो तुम काबिल हो?' विलंबित गायन का-सा अंदाज। व्यंग्य। 'जी!' लेकिन मुझे तो काबिल नहीं, होशियार आदमियों की जरूरत होती है!' लड़का कुछ समझा नहीं। बिटर-बिटर ताकने लगा। मित्तल ने समझाया - 'काबिल आदमी अच्छा काम कर सकता है, पर होशियार आदमी के मुकाबले में आता है तो बौखला जाता है और हार जाता है। होशियार आदमी चाहे उतना काबिल न हो, काबिल लोगों से अपना काम निकलवाना जानता है। कहिए? क्या कहते हैं?' लड़का मित्तल की बात का मतलब समझने की कोशिश करता रहा। 'और जिसे आप काबिलियत समझते हैं, वह क्या है?' मित्तल ने पूछा। लड़के से कोई जवाब देते नहीं बना। 'शायद आप कैशबुक बराबर मेंटेन कर सकते हैं, लेजर अपटुडेट रख सकते हैं, बैलेंस शीट पढ़ सकते हैं, एस्टीमेट ठीक से चैक कर सकते हैं, कॉस्ट शीट तैयार कर सकते हैं... पैसे-कौड़ी, लेन-देन, जमा-खर्च का हिसाब इतना साफ रख सकते हैं कि एक पैसे की भी गड़बड़ी न हो पाए।' 'जी, जी!' लड़का बोला। 'और जिसे अनाड़ी भी देखे तो उसकी समझ में आ जाए।' 'जी, जी!' लड़का उत्साहित हो उठा। 'और इसे आप काबिलियत समझते हैं!' लड़का फिर फक। मित्तल और आराम से पसर गए। बोले, 'समझिए, एक सोने का पहाड़ है हमारी इन्वेंटरी में। इसकी कीमत पता लगानी है। कैसे लगाएँगे?' 'सर, एक तरीका तो यह है कि बाजार भाव में उपलब्ध माल की मात्रा का गुणा कर दो... और अगर लागत मूल्य पता लगाना है तो...' 'सिंपल आनसर है। एक रुपया।' 'जी?' 'सोने के इस पहाड़ की कीमत एक रुपया!' 'जी, यदि असंप्शन ही करना है तो संभव है कि बुक बेल्यू...' 'मैं कहता हूँ एक रुपया!' इस बार मित्तल ने लगभग डाँटकर कहा। फिर बात को खोलते हुए कहा, 'मेरा अकाउंटेंट बोर्ड मीटिंग के ऐन पहले मेरे हुक्म के मुताबिक साल-भर के नफा-नुकसान, उत्पादन-बिक्री, जमा-खर्च के हिसाब हिसाब-किताब में गड़बड़ियाँ पैदा कर सकते हो या नहीं? अगर हाँ, तो कितनी देर में? और वह भी ऐसे कि गड़बड़ी में कोई गड़बड़ी न रहे!' लड़का फिर कोई जवाब नहीं दे पाया। 'अच्छा छोड़ो! यह बताओ कि जब इसी काबिलियत के पाँच आदमी और मिल रहे हों तो तुम्हीं को क्यों लिया जाए?' 'जी, मैं ईमानदार हूँ। आप आँख मूँदकर मुझ पर भरोसा कर सकते हैं।' मित्तल थोड़ा चौंके। फिर मुँह बिचकाकर बोले, 'अब तक तुम मुझे हँसा रहे थे, पर अब तो तुम मुझे डरा रहे हो। मैंने इतने साल में जो एंपायर खड़ी की है, उसे एक ईमानदार आदमी पर भरोसा करके मिट्टी में मिल जाने दूँ? क्या मेरा सिर फिर गया है? नहीं, शायद तुम मजाक कर रहे हो।' क्यों सर? ईमानदार होना कोई बुरी बात है क्या?' मित्तल साहब ने फिर बुरा-सा मुँह बनाया और खिड़की से बाहर देखने लगे। मानो सोच रहे हों - यह क्रासवर्ड पजल तो बहुत ही बोरिंग है! कुछ पल ऐसे ही बीत गए। लड़का हाथ धोने की तरह हाथ को हाथ से मलता रहा। रेलगाड़ी अब द्रुत ताल में चल रही थी। उसकी छकपक का सुर सध गया था और बात करने के लिए आवाज ऊँची नहीं करनी पड़ती थी। 'तुम्हारे कंसेप्ट बहुत पुराने हैं। कहीं तुम किसी अध्यापक के बेटे तो नहीं?' कुछ देर बाद मित्तल ने पूछा। लड़का क्या कहता? वह सचमुच अध्यापक का ही बेटा था। 'मेरी लड़की भी तुम्हारी ही तरह है। चौदह साल की हो गई, अब तक आदर्शवाद की चपेट में है। देखा जाए तो उसी के कारण मुझे तुम-जैसे... क्या कहना चाहिए... 'कल्पना पाखी' के साथ माथा खपाना पड़ रहा है। कहती है, जब डॉक्टरों ने मना कर रखा है तो मुझे हवाई जहाज में सफर नहीं करना चाहिए। उसे ने ये सारी, 'लंबे-चौड़े ताम-झाम की तरफ इशारा करते हुए, 'व्यवस्था की है। सारा कूपा मेरे लिए रिजर्व करा दिया। समझती नहीं कि डॉक्टर भी धंधा कर रहा है। अब कहिए?' लड़के को समझ में नहीं आया कि उसे क्या कहना है? मित्तल साहब ने फिर जेब से इलायची निकालकर मुँह में डाली और उसे दाढ़ से फोड़कर बोले, 'पहले कहा जाता था कि ईमानदारी से काम करना आदमी किताबों से सीखता है और बेईमानी से काम करना तजुरबे से। पर आज तो हमें इतना टाइम नहीं है कि आपको अनुभवी बनाने के लिए दस साल आपकी चाइल्डिश ईमानदारी भुगतें! आज तो इंडस्ट्री को ऐसे यंगस्टर्स चाहिए जो बेईमानी से काम करने में कुशल हों। जिसे कहते हैं प्रेग्मेटिक। इथिक्स की जगह चर्च में है, बिजनेस में नहीं। इसलिए ब्रीडिंग ही ऐसी होती है कि... अच्छे घरानों में बच्चों को बचपन से सिखाया जाता है, कैसे दूसरों से काम लेना... कब क्या बोलना, कब क्या नहीं बोलना... किसको मन की बात बताना, किसको नहीं... यानी तुम्हारी भाषा में बेईमानी कैसे करनी, चीटिंग कैसे करनी? खास स्कूलों में उन्हें भेजा जाता है... वहाँ सिखाया जाता है कि तुम्हारे काम क्या-क्या हैं, औरों के काम क्या-क्या हैं? तुम्हारे लिए सही-गलत क्या है, औरों के लिए सही-गलत क्या है, वगैरह। तो देखो, उन बच्चों के सामने कभी अंतरात्मा का संकट नहीं होता। दे आर रीयली ब्रिलिएंट एंड ऑफकोर्स सक्सेसफुल। इन मोस्ट ऑफ द केसेस।' 'लेकिन सर, ईमानदारी...??' 'कहाँ है ईमानदारी इस देश में? पॉलीटीशियंस? नौकरशाही? न्यायपालिका? पत्रकार? कलाकार? सामाजिक कार्यकर्ता? सामाजिक संस्थाएँ? कौन है ईमानदार? किसे जरूरत है आपकी ईमानदारी की?' 'लेकिन सर, ये ही तो सब कुछ नहीं है। देश में करोड़ों आदमी हैं। और वे बेईमान नहीं हैं। खेत में हल जोतता किसान, मशीन पर काम करता आदमी... गाँव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाता अध्यापक... सड़क पर झाड़ू लगाता मेहतर, रसोई में रोटी सेंकती औरत... क्या हम इन सबको बेईमान कह सकते हैं? और क्या हमारा देश इन लोगों की सम्मिलित बुद्धि, सम्मिलित बल से ही नहीं बनता? ईमानदारों के चर्चे नहीं होते। वे अखबारों की खबरें नहीं बनते। एक आदमी जेब काटता है... वह खबर बन जाता है... नौ सौ निन्यानवे आदमी जेब नहीं काटते। वे खबर नहीं बनते। क्या आसमान ऐसे ही टिका हुआ है सर! जरूर इतनी बड़ी चीज को उठाए रखने के लिए कुछ खंभे होते होंगे। ये लाखों-करोड़ों गुमनाम ईमानदार आदमी वैसे ही खंभे हैं सर!' लड़के की इस अचानक और चपल वक्तृता से मित्तल हतप्रभ रह गए। पैंतरा बदलकर बोले, 'देखो, कितने अच्छे विचार हैं तुम्हारे! कितने सुलझे हुए। तुम्हें तो पॉलिटिक्स करनी चाहिए।' लड़के को तुरंत अपनी भूल का एहसास हुआ और वह रुआँसा हो गया। मित्तल चुपचाप उसकी दुर्दशा का मजा लेते रहे। फिर बिस्किट निकालकर खाने लगे। लड़के से पूछा तक नहीं। कुछ देर बाद लड़का बोला, 'आयम सॉरी सर!' मित्तल के मुँह में बिस्कुट था। चबाना रुक गया। आँखें गोल-गोल हो गईं। जैसे पूछ रहे हों - क्यों-क्यों? गाड़ी धीमी हो गई। शायद कोई स्टेशन आ रहा था। अचानक लड़का उठा खड़ा हुआ। संकल्प की-सी मुद्रा में बोला, 'सर! मैं सक्सेसफुल बनूँगा। मैं बेईमान बनूँगा! बहुत बड़ा बेईमान! आप देखिएगा सर!' और बाहर जाने लगा। मित्तल आवाज मारकर बोले, 'फिर गलती कर गए। एक बात ध्यान से सुनो। किसी भी इंटरव्यू में जाओ, तो सारे सवालों के सही जवाब कभी मत देना। आते हों तो भी नहीं। वरना नौकरी देनेवाले को तुम पर एहसान करने का सुख कैसे मिलेगा? कुछ गुंजाइश छोड़ना उस बेचारे के लिए भी। इसके अलावा कोई भलाई का काम उसे नहीं आता।' लड़का बगैर कोई जवाब दिए चला गया और उतर गया। मित्तल अदम्य सुख से मुस्कराए। उन्होंने सोचा - अब लड़का अगर उनसे मिलने आया - आ सकता है - तो वे जरूर उसे मित्री से मिलवाएँगे। मित्री को अच्छा लगेगा। बल्कि उनकी तो इच्छा है कि मित्री अपने लिए ऐसा ही कोई लड़का पसंद करे। बजरबट्टू। इसका भविष्य उज्ज्वल है। ढंग की ट्रेनिंग मिल गई तो आगे जाकर अच्छा बेईमान बन सकता है। ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🖥 प्रस्तुति - Uniting Working Class 👉 *हर दिन कविता, कहानी, उपन्यास अंश, राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक विषयों पर लेख, रविवार को पुस्तकों की पीडीएफ फाइल आदि व्हाटसएप्प, टेलीग्राम व फेसबुक के माध्यम से हम पहुँचाते हैं।* अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इस लिंक पर जाकर हमारा व्हाटसएप्प चैनल ज्वाइन करें - https://www.mazdoorbigul.net/whatsapp चैनल ज्वाइन करने में कोई समस्या आए तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख कर भेज दें - 8828320322 🖥 फेसबुक पेज - https://www.facebook.com/mazdoorbigul/ https://www.facebook.com/unitingworkingclass/ 📱 टेलीग्राम चैनल - http://www.t.me/mazdoorbigul हमारा आपसे आग्रह है कि तीनों माध्यमों व्हाट्सएप्प, फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ें ताकि कोई एक बंद या ब्लॉक होने की स्थिति में भी हम आपसे संपर्क में रह सकें।

📚 *देश-दुनिया का बेहतरीन साहित्य* 📚 _________________________ *येह शेङ ताओ की प्रसिद्ध कहानी - नंगा राजा* 📱https://www.mazdoorbigul.net/archives/5565 👉 English version of this story was not available on internet (In text format). We have uploaded text this time. English Version is taken from Chinese literature, 1954-3. To read this please visit above link. --------------------------- बहुत से लोगों ने नये-नये कपड़े पहनने के शौक़ीन उस राजा के बारे में हैन्स एण्डर्सन की कहानी पढ़ी होगी जिसे एक बार दो ठगों ने उल्लू बना दिया था। उन ठगों ने यह दावा किया कि वे राजा के लिए ऐसी सुन्दर पोशाक़ तैयार करेंगे जैसी कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। पर सबसे बड़ी ख़ूबी उसमें यह होगी कि वह पोशाक़ किसी मूर्ख व्यक्ति या अपने पद के लिए अयोग्य व्यक्ति को दिखायी नहीं देगी। राजा ने तुरन्त अपने लिए ऐसी पोशाक़ बनाने को आदेश दे दिया और दोनों ठग बुनने, काटने और सिलने का अभिनय करने में जुट गये। राजा ने कई बार अपने मन्त्रियों को काम की रफ़्तार देखने के लिए भेजा और हर बार उन्होंने उसे बताया कि वे अपनी आँखों से नये वस्त्रें को देखकर आ रहे हैं और वे वाकई बेहद ख़ूबसूरत हैं। दरअसल, राजा के मन्त्रियों ने कुछ भी नहीं देखा था, पर वे मूर्ख कहलाना नहीं चाहते थे और उससे भी बढ़कर अपने पदों के लिए अयोग्य घोषित किया जाना तो नहीं ही चाहते थे। राजा ने तय किया कि जिस दिन नयी पोशाक़ तैयार हो जायेगी, उस दिन एक भव्य समारोह होगा और राजा नयी पोशाक़ पहनकर नगर में निकलेगा। राज्यभर में इसकी मुनादी करवा दी गयी। जब वह दिन आया तो ठगों ने राजा के सारे कपड़े उतरवा दिये। फिर वे देर तक उसे नये परिधान में सजाने-धजाने का अभिनय करते रहे। राजा के दरबारियों और नौकर-चाकरों ने एक स्वर में उसकी तारीफ़ों के पुल बाँधने शुरू कर दिये क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि वे मूर्ख कहलायें या अपने पदों के लिए अयोग्य घोषित कर दिये जायें। राजा ने सन्तुष्ट भाव से सर हिलाया और नंगधड़ंग बाहर चल पड़ा। रास्ते के दोनों तरफ़ खड़े लोग भी मूर्ख कहलाना नहीं चाहते थे। वे सब के सब राजा की नयी पोशाक़ की इस तरह से प्रशंसा कर रहे थे जैसे वे उसे साफ़-साफ़ देख रहे हों। लेकिन तभी एक बच्चा बड़ी मासूमियत से बोल पड़ा, “अरे, उस आदमी ने तो कुछ पहना ही नहीं है!” भीड़ के कानों में यह बात पड़ते ही चारों तरफ़ फैल गयी और जल्दी ही हर आदमी हँस रहा था और चिल्ला रहा थाः “अरे सच! राजा के बदन पर एक सूत भी नहीं है।” अचानक राजा की समझ में आया कि उसे धोखा दिया गया है। लेकिन अब तो खेल शुरू हो चुका था और उसे बीच में रोकने का मतलब होता, और बेइज़्ज़ती। उसने तय किया कि वह इसे जारी रखेगा और सीना फुलाकर आगे चल दिया। इसके बाद क्या हुआ? हैन्स एण्डर्सन ने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, लेकिन दरअसल इस कहानी में और भी बहुत कुछ हुआ था। राजा अपने भव्य जुलूस के साथ आगे चलता रहा, मानो कुछ हुआ ही न हो। और वह इतना अकड़कर चल रहा था कि उसके कन्धे और रीढ़ की हड्डी तक दुखने लगे। उसकी अदृश्य पोशाक़ के पिछले भाग को उठाकर चलने का अभिनय कर रहे सेवक बड़ी मुश्किल से अपने होंठ चबा-चबाकर हँसी रोक रहे थे क्योंकि वे मूर्ख कहलाना नहीं चाहते थे। अंगरक्षक अपनी निगाहें जमीन पर गड़ाये हुए चल रहे थे क्योंकि अगर किसी एक की भी नज़र अपने साथी से मिल जाती तो उसके मुँह से जरूर हँसी फूट पड़ती। लेकिन जनता तो ज़्यादा स्पष्टवादी होती है। उसे अपने होंठ काटने और निगाहें ज़मीन पर गड़ाये रखने की कोई वजह समझ में नहीं आयी। इसलिए जब एक बार यह नंगी सच्चाई उजागर हो गयी कि राजा कुछ नहीं पहने है, तो वे ज़ोर-ज़ोर से ठहाके लगाकर हँसने लगे। “अच्छा राजा है यह तो, नंगधड़ंग चला जा रहा है,” एक ने खिलखिलाते हुए कहा। “ज़रूर इसकी अकल घास चरने चली गयी है,”” दूसरे ने कहकहा लगाया। “थुलथुल, बदसूरत कीड़ा,” किसी ने फब्ती कसी।” ““उसके कन्धे और टांगें देखे, जैसे पंख नुची हुई मुर्गी,”” चौथे आदमी ने ताना मारा। इन फ़ब्तियों से राजा का ग़ुस्सा भड़क उठा। उसने जुलूस रोक दिया और अपने मन्त्रियों को डपटा, “सुना तुमने, इन मूर्खों और देशद्रोहियों की ज़ुबान बहुत चलने लगी है। तुम लोग रोकते क्यों नहीं उन्हें? मेरे नये वस्त्र बहुत ठाठदार हैं और इन्हें पहनने से मेरी राजसी आनबान बढ़ती है। तुम लोग ख़ुद यह बात कह रहे थे। आज से मैं सिर्फ़ यही कपड़े पहनूँगा और दूसरा कुछ नहीं पहनूँगा। जो कोई यह कहने की हिम्मत करता है कि मैं नंगा हूँ, वह दुष्ट और ग़द्दार है। उसे फ़ौरन गिरफ़्तार करके मौत के घाट उतार दिया जाये। यह एक नया क़ानून है। इसकी घोषणा फ़ौरन कर दी जाये।”” राजा के मन्त्री तुरन्त भागदौड़ करने लगे। नगाड़े पीटकर प्रजा को इकट्ठा किया गया और मन्त्रियों ने पूरी ताक़त से चिल्ला-चिल्लाकर इस नये क़ानून की घोषणा कर दी। हँसना और फब्तियाँ कसना बन्द हो गया और राजा ने सन्तुष्ट होकर जुलूस को आगे बढ़ने का आदेश दिया। लेकिन वह अभी थोड़ी ही दूर गया था कि ठहाकों और फ़ब्तियों की आवाजें उसके कानों में पटाखों की तरह गूँजने लगी। ““उसके बदन पर एक सूत भी नहीं है।”” “कैसा घिनौना पिलपिला बदन है।”” ““उसकी तोंद देखो, जैसे सड़ा हुआ कद्दू!”” ““उसके नये कपड़े वाक़ई कमाल के हैं!”” हर ताने के साथ ज़ोरदार कहकहे लगते थे। राजा फिर भड़क गया। उसने खा जाने वाली नज़रों से मन्त्रियों को घूरा और चिंघाड़ा, ““इसे सुना तुमने!”” “हाँ महाराज, हमने सुना इसे,”” काँपते हुए मन्त्रियों ने जवाब दिया। “क्या तुम भूल गये अभी-अभी मैंने क्या नया क़ानून बनाया है?”” राजा की बात पूरी होने का इन्तज़ार किये बिना मन्त्रियों ने सिपाहियों को आदेश दिया कि उन सबको गिरफ़्तार कर लायें जो हँस रहे थे या फ़ब्तियाँ कस रहे थे। चारों तरफ़ भगदड़ मच गयी। सिपाही इधर से उधर दौड़ने लगे और भागने की कोशिश कर रहे लोगों को अपने बल्लमों से रोकने लगे। बहुत से लोग गिर पड़े, कुछ दूसरों के ऊपर से छलाँग मारकर भागने में सफल हो गये। फ़ब्तियों और हँसी की जगह चीख़ें और सिसकियाँ सुनाई पड़ने लगीं। क़रीब पचास लोग पकड़े गये और राजा ने उनको वहीं मार डालने का हुक्म दिया ताकि प्रजा समझ जाये कि उसके मुँह से निकली बात लौह क़ानून है और कोई उसका मज़ाक नहीं उड़ा सकता। उस दिन के बाद से राजा ने कोई कपड़ा नहीं पहना। अन्तःपुर से लेकर दरबार तक, हर जगह वह नंगा ही जाता था और बीच-बीच में अपनी पोशाक़ की सिलवटें ठीक करने का अभिनय करता रहता था। उसकी रानियाँ और दरबारी शुरू-शुरू में उसे अपने बदसूरत पिलपिले शरीर के साथ घूमते और ऐसी हरक़तें करते देखकर मज़ा लेते थे, पर धीरे-धीरे वे ऐसा दिखावा करना सीख गये जैसे कोई बात ही न हो। वे इसके आदी हो गये और अब वे राजा को ऐसे ही देखते थे जैसे वह पूरी तरह कपड़े पहने हुए हो। रानियाँ और दरबारीगण इसके सिवा कुछ कर भी नहीं सकते थे, अन्यथा वे अपने पदों से और यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ धो बैठते। लेकिन इतनी जीतोड़ कोशिशों के बावजूद एक पल की गफलत भी उनके सर्वनाश का कारण बन सकती थी। एक दिन राजा की प्रिय रानी उसे ख़ुश करने के लिए अपने हाथों से सुरापान करा रही थी। उसने लाल शराब का एक प्याला भरकर राजा के होठों से लगाया और ख़ूब मीठे स्वर में बोली, “इसे पीजिये और ईश्वर करे कि आप हमेशा जीवित रहें।” राजा इतना ख़ुश हुआ कि उसने एक साँस में प्याला खाली कर दिया। लेकिन इसने शायद कुछ ज़्यादा ही जल्दी कर दी क्योंकि उसे खाँसी आ गयी और शराब उसकी छाती पर बह चली। “अरे आपकी छाती पर धब्बा लग गया है,” रानी बोल पड़ी। “क्या, मेरी छाती पर!”” अपनी भूल का अनुभव करते ही राजा की प्रिय रानी का चेहरा पीला पड़ गया। “नहीं, आपकी छाती पर नहीं,”” उसने काँपते हुए स्वर में अपनी भूल सुधारी, ““आपकी पोशाक़ पर धब्बा लग गया है।”” “तुमने कहा कि मेरी छाती पर धब्बा लग गया है। यह वही बात हुई कि मैं कुछ भी नहीं पहने हूँ। बेवकूफ़ कहीं की! तू दग़ाबाज़ है और तूने मेरा क़ानून तोड़ा है!”” इतना कहने के साथ ही राजा चिल्लाया, “ले जाओ इसे जल्लाद के पास।”” और उसके सिपाही रानी को घसीट ले गये। राजा का एक बहुत विद्वान मन्त्री भी राजा की सनक का शिकार हुआ। हालाँकि उसने भी सबकुछ अनदेखा करने की आदत डाल ली थी, लेकिन उसे भरे दरबार में एक ऐसे आदमी को राजा कहने में शर्म आती थी, जो गद्दी पर बिलकुल नंगा बैठता था। मन ही मन वह उसे ‘गंजा बन्दर’ कहता था। वह डरता था कि यदि किसी दिन उसके मुँह से असावधानीवश कोई बात निकल गयी या वह किसी ग़लत मौक़े पर हँस पड़ा तो उसकी बरबादी निश्चित है। इसलिए उसने अपनी बूढ़ी माँ को देखने घर जाने के बहाने से राजा से छुट्टी माँगी। राजा ने कहा कि, “मैं किसी मातृभक्त बेटे की प्रार्थना भला कैसे ठुकरा सकता हूँ।”” और उसे जाने की छुट्टी दे दी। मन्त्री को उस समय ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसे मोटी-मोटी ज़ंजीरों से मुक्ति मिल गयी हो। उसने राहत की साँस ली और उसके मुँह से धीरे से निकल गया, “भगवान का लाख-लाख शुक्र है, अब मुझे उस नंगे राजा की ओर देखना नहीं पड़ेगा।”” राजा के कान में भनक पड़ी तो उसने अपने सेवकों से पूछा, “क्या कहा उसने?”” सेवक हड़बड़ी में कोई बात बना नहीं पाये और उन्होंने उसे पूरी बात बता दी। ““अच्छा तो तुमने इसलिए छुट्टी माँगी थी क्योंकि तुम मुझे देखना बरदाश्त नहीं कर सकते,”” राजा चिल्लाया। “तुमने मेरा क़ानून तोड़ा है। अब देखो मैं ऐसा इन्तज़ाम करता हूँ कि तुम घर पहुँच ही न पाओ।”” इसके बाद उसने अपने जल्लादों को हुक्म दिया कि वे मन्त्री को ले जायें और उसकी गरदन उड़ा दें। इन घटनाओं के बाद अन्तःपुर और दरबार में हर आदमी और ज़्यादा चौकन्ना हो गया। लेकिन आम जनता ने तो रानियों और दरबारियों जैसी चालाकी नहीं सीखी थी। जब भी राजा लोगों के सामने आता था और वे उसके ढोंग को और उसके भद्दे शरीर को देखते थे, वे हँसी रोक नहीं पाते थे। इसके बाद खूनी हत्याओं का सिलसिला शुरू हो जाता था। एक दिन जब राजा मन्दिर में यज्ञ करने के लिए गया तो उसके सिपाहियों ने तीन सौ लोगों को जल्लाद के हवाले किया। जिस दिन वह अपने सैनिकों का मुआयना करने निकला उस दिन पाँच सौ लोग मौत के घाट उतारे गये, और एक दिन जब वह राज्य के शाही दौरे पर निकला तो राज्य भर में हजारों लोग मारे गये। एक दयालु बूढ़े मन्त्री ने सोचा कि राजा हद से बाहर जा रहा है और अब यह सब बन्द होना चाहिए। लेकिन राजा यह कभी नहीं मानता कि वह ग़लत है। उससे उसकी ग़लती बताना अपने गले में फन्दा डालने के समान था। बूढ़े मन्त्री ने सोचा कि अगर किसी तरह से राजा को फिर से कपड़े पहना दिये जायें तो जनता की हँसी और फ़ब्तियाँ रुक जायेंगी और लोगों की जान बचेगी। कई रातों तक जाग-जागकर वह सोचता रहा कि क्या करे जिससे साँप भी मर जाये और लाठी भी न टूटे। आख़िर उसे एक योजना सूझी और वह राजा के पास गया। उसने कहा, “मेरे मालिक! आपके एक वफ़ादार सेवक के नाते मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। आप हमेशा नये-नये कपड़ों के शौक़ीन रहे हैं क्योंकि उनसे आपकी शानशौक़त को चार चाँद लग जाते हैं। लेकिन इधर बहुत दिनों से आप राज्य के मामलों में इतने व्यस्त रहे हैं कि आपको नये कपड़ों का ध्यान ही नहीं रहा है। जो पोशाक़ आपने पहनी हुई है, उसका रंग फीका पड़ रहा है। आप अपने दर्जियों को आदेश दीजिये कि वे आपके लिए एक नयी और शानदार पोशाक़ बनाकर तैयार करें।” “क्या कहा, मेरी पोशाक़ का रंग फीका पड़ रहा है?”” उसने अपने शरीर पर हाथ फिराते हुए कहा। “बकवास! ये जादुई पोशाक़ है। इसका रंग कभी फीका नहीं पड़ सकता। तुमने सुना नहीं, मैंने कहा था कि अब मैं इसके सिवा और कुछ नहीं पहनूँगा। तुम चाहते हो कि मैं इसे उतार दूँ, ताकि मैं भद्दा दिखूँ! चलो, तुम्हारी उम्र और तुम्हारी पिछली सेवाओं का ख़्याल करके तुम्हारी जान बख़्श दे रहा हँ, लेकिन तुम्हारी बाक़ी ज़िन्दगी अब जेल में कटेगी।”” सैकड़ों निर्दोषों को प्राणदण्ड देने का क्रम चलता रहा। उल्टे, लोगों की हँसी बन्द न होने से राजा एकदम तुनक गया और उसने और भी ज़्यादा कड़ा क़ानून बना दिया। इस बार उसने फ़रमान जारी कर दिया कि जब राजा सड़क पर निकले उस वक़्त कहीं से किसी आदमी की किसी भी तरह की आवाज़ नहीं आनी चाहिये। अगर किसी ने कोई आवाज़ निकाली तो उसे हाथी से कुचलवा दिया जायेगा। इस क़ानून की घोषणा के बाद राज्यभर के गणमान्य नागरिक सोचने लगे कि अब तो राजा अति कर रहा है। ठीक है कि राजा की हँसी उड़ाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन दूसरी चीज़ों के बारे में बात करने पर क्यों प्राणदण्ड दिया जाये? वे सब जुलूस बनाकर राजा के यहाँ गये और राजमहल के बाहर घुटनों के बल झुककर बोलो कि वे राजा को एक अर्ज़ी देने आये हैं। घबराया हुआ राजा बाहर आया और गरजकर बोला, “तुम लोग यहाँ क्या करने आये हो? बग़ावत करना चाहते हो?”” गणमान्य नागरिकों ने अपने सर उठाने की जुर्रत किये बिना जल्दी से जवाब दिया, “नहीं, नहीं महाराज, आप हमें ग़लत समझ बैठे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं।”” राहत महसूस करते हुए राजा ने शान से अपनी अदृश्य पोशाक़ की सलवटें ठीक कीं और पहले से भी ज़्यादा कड़ी आवाज में बोला, “फिर तुम लोग इतनी भीड़ बनाकर यहाँ क्यों आये हो?”” “हम महाराज से प्रार्थना करने आये हैं कि हमारी हँसने-बोलने की आज़ादी लौटा दी जाये। जो आप पर कीचड़ उछालते हैं और हँसी उड़ाते हैं, वे दुष्ट लोग हैं और उनको ज़रूर मार डालना चाहिए। मगर हम सब लोग राजभक्त, ईमानदार नागरिक हैं, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप अपना नया क़ानून वापस ले लें।”” ““आज़ादी? और तुम लोगों को? अगर तुम आज़ादी चाहते हो तो मेरी प्रजा नहीं रह सकते। अगर तुम मेरी प्रजा रहना चाहते हो तो मेरे क़ानूनों को मानना पड़ेगा। और मेरे क़ानून लोहे जैसे सख़्त हैं। उन्हें मैं वापस ले लूँ? कभी नहीं!”” – इतना कहने के साथ ही राजा पलटा और अपने महल में चला गया। नागरिकों को इससे आगे कहने की हिम्मत नहीं हुई। डरते-डरते उन्होंने धीरे से सर उठाया और देखा कि राजा जा चुका है। अब वे वापस घर लौटने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। इसके बाद से लोगों ने एक नया तरीक़ा अपना लिया – जब राजा बाहर आता था, तब वे बन्द दरवाजों के पीछे अपने घरों में ही क़ैद रहते थे, सड़कों पर झाँकते तक नहीं थे। एक दिन राजा अपने मन्त्रियों और अंगरक्षकों के साथ महल से बाहर अपनी आरामगाह के लिए चला। सारी सड़कें सूनी पड़ी थीं और दोनों तरफ़ घरों के दरवाजे बन्द थे। जो अकेली आवाज़ उन्हें सुनायी दे रही थी वह उनके अपने पैरों की पदचाप थी, जैसे रात के सन्नाटे में कोई सेना मार्च कर रही हो। तभी अचानक राजा थम गया और कान खड़े करते हुए अपने मन्त्रियों पर गरजा, फ्सुन रहे हो ये आवाज़?” मन्त्रियों ने भी सुनने के लिए कान लगा दिये। “हाँ, एक बच्चा रो रहा है,”” एक बोला। ““एक औरत गा रही है,”” दूसरे ने बताया। “वह आदमी ज़रूर नशे में धुत्त होगा, बदमाश कहीं का, खिलखिलाकर हँस रहा है,”” तीसरे मन्त्री ने कहा। अपने मन्त्रियों को सारा मामला इतना हल्का बनाते देखकर राजा आगबबूला हो गया। “क्या तुम लोग मेरा नया क़ानून भूल गये हो?”” – वह पूरी ताक़त से चिंघाड़ा। ग़ुस्से के मारे उसकी आँखें बाहर निकली पड़ रही थीं और उसका थुलथुल सीना धौंकनी की तरह चल रहा था। मन्त्रियों ने तुरन्त सिपाहियों को हुक्म दिया कि घरों में घुस जायें और जिस किसी ने भी कोई भी आवाज़ निकाली हो – चाहे वह बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत कोई भी हो – उसे पकड़ लायें और जल्लाद के हवाले कर दें। लेकिन तभी ऐसी घटना घटी जिसकी राजा ने सपने में भी आशा नहीं की थी। जब सिपाहियों ने घरों के दरवाज़े तोड़े तो औरतों, पुरुषों और बच्चों का हुजूम बाहर उमड़ पड़ा। वे राजा की ओर झपटे और हाथों को बाज़ के पंजों की तरह ताने हुए उसके शरीर पर टूट पड़े। वे चिल्ला रहे थे, “नोच डालो! इसकी ख़ूनी पोशाक़ को नोच डालो!”” आदमियों ने राजा की बाँहें पकड़कर मरोड़ दीं। औरतें उसकी छाती और पीठ पर मुक्के बरसा रही थीं। दो छोटे बच्चे उसकी बाँहों के नीचे और पेट में गुदगुदी मचा रहे थे। चारों तरफ़ से घिर चुके राजा को भागने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उसने अपना सिर घुटनों में छिपा लिया और गिलहरी की तरह गुड़ीमुड़ी हो गया, लेकिन सब बेकार। उसकी बगलों में मच रही भयानक गुदगुदी और उसके पूरे बदन में हो रही जलन उसकी बरदाश्त के बाहर हो रहे थे। वह किसी भी तरह इस मुसीबत से छुटकारा नहीं पा सकता था। उसने अपना सिर कंधें में दुबका लिया और उसके मुँह से क्रोध, भय और हैरानी की मिलीजुली ध्वनियाँ निकलने लगीं। उसके भृकुटि तानने और उन्हें डराने-धमकाने के प्रयासों को देखकर लोगों का हँसी के मारे बुरा हाल हो गया। लोगों के घरों से निकलते हुए सिपाहियों ने देखा कि राजा कितना मज़ाकिया लग रहा था – जैसे क्रुद्ध बर्रों से घिरा बन्दर – तो वे भूल गये कि उन्हें उसके प्रति सम्मान दिखाना चाहिए और वे भी सबके साथ हँसी में शामिल हो गये। इसे देखकर पहले तो मन्त्रीगण डर गये, लेकिन फिर उन्होंने कनखी से राजा की ओर देखा और वे सब भी ठहाका मारकर हँस पड़े। हँसते-हँसते दोहरे हुए जाते मन्त्रियों के दिमाग में अचानक यह बात आयी कि वे राजा का क़ानून तोड़ रहे हैं और उन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। इसके पहले जब जनता राजा की खिल्ली उड़ाती थी तो मन्त्री ही उसे दण्ड दिया करते थे और अब वे खुद उस पर हँस रहे थे। तभी उन्होंने उसकी तरफ़ फिर ध्यान से देखा। उसके पूरे शरीर पर काले-काले चकत्ते पड़े हुए थे और वह गठरी बना हुआ ऐसा लग रहा था जैसे बरसात में भीगा हुआ मुर्गी़ का बच्चा। उसे देखते ही हँसी छूट रही थी। “क्या यह स्वाभाविक नहीं है कि लोग मज़ाकिया चीज़ों पर हँसें? लेकिन राजा ने तो क़ानून बनाकर लोगों के हँसने पर पाबन्दी लगा दी थी। क्या बेहूदा क़ानून है!”” और मन्त्री भी लोगों के साथ मिलकर चिल्लाने लगे “नोच डालो! इसके झूठे कपड़ों को नोच डालो!”” जब राजा ने देखा कि उसके मन्त्री और सिपाही भी जनता से मिल गये हैं और अब वे उससे जरा भी खौफ़ नहीं खा रहे हैं तो उसे ऐसा धक्का लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर भारी हथौड़ा दे मारा हो, और वह चारों खाने चित्त, धरती पर जा गिरा। ➖➖➖➖➖➖➖➖ 🖥 प्रस्तुति - Uniting Working Class 👉 *हर दिन कविता, कहानी, उपन्यास अंश, राजनीतिक-आर्थिक-सामाजिक विषयों पर लेख, रविवार को पुस्तकों की पीडीएफ फाइल आदि व्हाटसएप्प, टेलीग्राम व फेसबुक के माध्यम से हम पहुँचाते हैं।* अगर आप हमसे जुड़ना चाहें तो इस लिंक पर जाकर हमारा व्हाटसएप्प चैनल ज्वाइन करें - http://www.mazdoorbigul.net/whatsapp चैनल ज्वाइन करने में कोई समस्या आए तो इस नंबर पर अपना नाम और जिला लिख कर भेज दें - 8828320322 🖥 फेसबुक पेज - https://www.facebook.com/mazdoorbigul/ https://www.facebook.com/unitingworkingclass/ 📱 टेलीग्राम चैनल - http://www.t.me/mazdoorbigul हमारा आपसे आग्रह है कि तीनों माध्यमों व्हाट्सएप्प, फेसबुक और टेलीग्राम से जुड़ें ताकि कोई एक बंद या ब्लॉक होने की स्थिति में भी हम आपसे संपर्क में रह सकें।