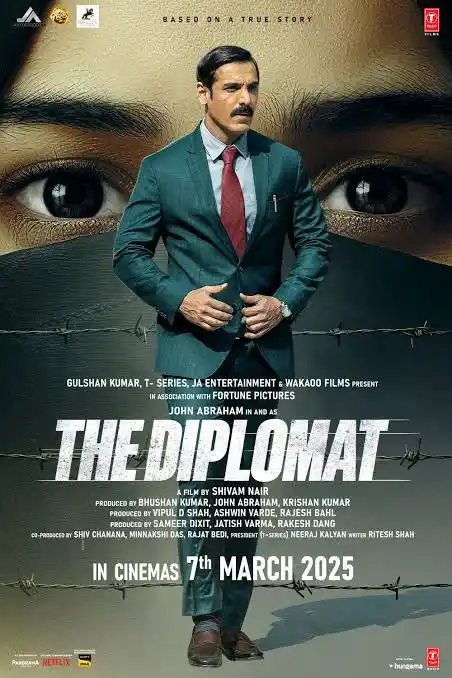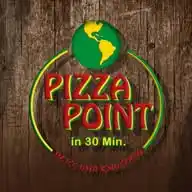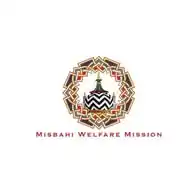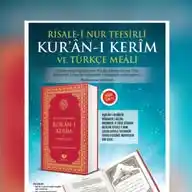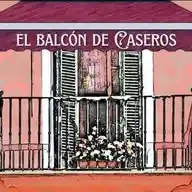सुलेखसंवाद
144 subscribers
About सुलेखसंवाद
पढ़ने की आदत डालिये लिखे हुए से संवाद करना सबसे बेहतरीन संवाद होता है। यहाँ आपको केवल और केवल पढ़ने और समझने की सीख के लिए साहित्य का परिचय दिया जाएगा। हिंदी, अंग्रेज़ी मैथिली में। शेष आगे देखते हैं क्या हो पाएगा उद्देश्य केवल विवेक और विज्ञान सम्मत चेतना का निर्माण है।
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

🔎 भाषा का लोकतंत्रीकरण: बनाम शुद्धिकरण राजस्थान सरकार ने हाल ही में पुलिस और प्रशासनिक संवादों से उर्दू व फ़ारसी मूल के शब्दों को हटाकर “सरल हिंदी” शब्दों को अपनाने का निर्देश दिया है। तर्क दिया गया कि ये शब्द “मुग़लकालीन” पृष्ठभूमि से जुड़े हैं और आम जनता या नव-नियुक्त कर्मियों द्वारा ठीक से नहीं समझे जाते। लेकिन यह कदम दो बातों को समझने की मांग करता है। यह भाषा का सरलीकरण है या शुद्धिकरण? सरलीकरण और शुद्धिकरण में राजनीतिक आयाम का अंतर है काफी बड़ा अंतर और इस बहस के केंद्र में जो बात सबसे कम चर्चा में आती है, वह है – 👉 भाषा का लोकतंत्रीकरण। 🧭 भाषा का लोकतंत्रीकरण क्या है? भाषा का लोकतंत्रीकरण मतलब यह नहीं कि भाषा “सरल” हो जाए, बल्कि यह कि हर व्यक्ति को भाषा तक समान पहुंच, समझ और उपयोग की क्षमता मिले — चाहे वह किसी वर्ग, जाति, लिंग, या समुदाय से आता हो। •एक लोकतांत्रिक समाज में भाषा संपर्क का माध्यम बनती है, दीवार नहीं। •यह जनता को सशक्त करती है, हाशिए पर नहीं धकेलती। •यह भाषा भाषिक विविधता को अपनाती है, उसे संकीर्ण परिभाषाओं में सीमित नहीं करती। 📚 हिंदी और उर्दू: एक साझी विरासत हिंदी और उर्दू की उत्पत्ति एक ही सामाजिक-सांस्कृतिक भूमि से हुई — खड़ी बोली। •हिंदी ने संस्कृतनिष्ठ साहित्यिक रंग अपनाया, •जबकि उर्दू ने फारसी-तुर्की-अरबी शब्दावली से समृद्ध होकर एक दरबारी व साहित्यिक रूप लिया। लेकिन आम हिंदुस्तानी जनजीवन में दोनों की मिलीजुली भाषा रही — जिसे कभी हिंदुस्तानी कहा गया। गांधी जी ने इसी भाषा को भारत की संपर्क भाषा मानने की वकालत की थी “हिंदुस्तानी वह भाषा होगी जो हिंदी और उर्दू दोनों को अपनाएगी।” 🔍 उर्दू शब्द हटाने का निर्णय: क्या वास्तव में “सरलता” का सवाल है? राजस्थान सरकार के फैसले के बाद पुलिस संवादों से जिन शब्दों को हटाया जा रहा है, वे कुछ इस तरह के हैं: या होंगे .. गवाह, मुक़दमा, इलज़ाम, इत्तिला, रोज़नामा, मुल्ज़िम आदि। वास्तविकता यह है कि ये शब्द कानूनी और सामाजिक संवाद का हिस्सा बन चुके हैं। •आम जनता “गवाह” को तो समझती है, पर “साक्षी” कहने से क्या संवाद और पारदर्शी हो जाएगा? • क्या “इलज़ाम” शब्द आम जीवन से इतना अलग है कि उसे हटाना जरूरी हो? यदि उद्देश्य “समझ को आसान बनाना” है, तो सवाल उठता है कि अंग्रेज़ी या संस्कृतनिष्ठ शब्द क्या सरल समझे जाते हैं कितने लोग नीचे लिखे शब्दों का अर्थ समझते हैं ? उदाहरण के लिए: • प्रावधान, अधिनियम, परिवीक्षा, धारा, प्रवर्तन निदेशालय – क्या ये आमजन सहज समझते हैं? 🧠 समस्या भाषा नहीं, प्रशिक्षण और साक्षरता की है हमारी न्याय और प्रशासन व्यवस्था में समस्या शब्दों की नहीं, बल्कि भाषिक प्रशिक्षण की अनुपस्थिति की है। • पुलिस, चिकित्सा, कानून और विज्ञान – इन सभी क्षेत्रों में तकनीकी भाषा का प्रयोग आवश्यक है, लेकिन उसकी लोकप्रशिक्षण व्यवस्था लगभग शून्य है। • यदि कोई डॉक्टर “हृद्गत संकुचन” बोले, तो क्या आम नागरिक उसे समझेगा? “दिल का दौरा” कहना ही संप्रेषण के लोकतंत्रीकरण का उदाहरण है। 🇮🇳 एक समावेशी हिंदी की ज़रूरत हिंदी यदि सच में भारत की संपर्क भाषा बननी है, तो उसे उर्दू, अंग्रेज़ी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, दक्षिण भारतीय भाषाओं से शब्द लेकर अपने को समृद्ध करते रहना होगा। हिंदी कोई शुद्ध संस्कृत नहीं है। वह बोलियों का संगम है, इतिहास का दर्पण है, और लोक की भाषा है। “हिंदी को ‘शुद्ध’ करने की चाह, उसे ‘अजनबी’ बना देती है।” ✅ समाधान क्या हो सकता है? 1. जनभाषा को तकनीकी भाषा से जोड़ने के प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएं – विशेष रूप से पुलिस, स्वास्थ्य और कानून के क्षेत्र में। 2. द्विभाषिक शब्दावली को अपनाया जाए – जैसे “गवाह (साक्षी)”, “इलज़ाम (आरोप)” आदि। 3. भाषा को राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रतीक की बजाय जनसंचार का माध्यम माना जाए। ✍️ निष्कर्ष: भाषा का लोकतंत्रीकरण ही सच्चा राष्ट्रवाद है राजस्थान सरकार का निर्णय “सरलता” के नाम पर कहीं सांस्कृतिक शुद्धिकरण का अभ्यास न बन जाए। यह जन के लिए नहीं, एक खास राजनीतिक अभिकथन (क्या आप अभिकथन का अर्थ जानते हैं नहीं जानते होंगे नैरेटिव सुना होगा) लिए भाषा को ढालने का प्रयास है। यदि हमें भाषा को लोकतांत्रिक बनाना है, तो हमें शब्दों को मिटाना नहीं, अर्थों को जोड़ना होगा। हिंदी तभी मजबूत होगी जब वह सबकी हिंदी बने — जिसमें “गवाह” भी हो, “साक्षी” भी, और “विटनेस” भी। तभी हम कह सकेंगे कि हमारी भाषा, हमारी है — सबकी है, समावेशी है और उसे सशक्त साबित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।

“धर्म का अवशेष या अंधविश्वास का प्रचार — हादसे की राख में पवित्रता का स्वांग” जब किसी विमान दुर्घटना में सैकड़ों जानें चली जाती हैं, और उसके मलबे में से एक धार्मिक पुस्तक जली नहीं मिलती — तो हमारे समाज का ध्यान सुरक्षा नीति, प्रशासनिक विफलताओं या मानवीय त्रुटियों पर नहीं, उस ‘चमत्कार’ पर चला जाता है। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज़ आती है — “देखिए, सब कुछ जल गया, लेकिन गीता/कुरान/बाइबिल सही-सलामत है!” यह वही समाज है जो हर मंदिर/मस्जिद/गिरिजाघर में सीसीटीवी लगवाकर ईश्वर की निगरानी करता है, लेकिन विमान तकनीकी जांच की बजाए धार्मिक ग्रंथ की अक्षतता को दैवी प्रमाण मान लेता है। क्या यह अध्यात्म है? नहीं, यह पाखंड है — सुनियोजित, मनोरंजनात्मक, और जन मानस को तर्कशक्ति से दूर धकेलने वाला पाखंड। 📜 सदियों से धर्म ने मनुष्य को आत्म-निरीक्षण, करुणा और न्याय की ओर उन्मुख करने की कोशिश की है। भगवद्गीता युद्ध के मैदान में खड़ी होकर भी शांति का पाठ पढ़ाती है। पर जब हम इन पुस्तकों को ‘अग्नि में न जलने’ की प्रतियोगिता में शामिल कर देते हैं, तो हम इनके मूल संदेश को नष्ट कर रहे होते हैं — किताबें नहीं जलतीं, विचार जलाए जा रहे होते हैं। 🧠 यह ‘महिमा’ का आख्यान उस समाज में पनपता है जहाँ विफलताओं का बोझ जनता पर डालने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। ट्रेन पलट जाए, तो बोला जाता है कि किसी साधु को ठेस पहुँचाई गई थी। भवन गिर जाए, तो कहा जाता है कि ज़मीन पर देवता का अपमान हुआ था। यह रणनीति है — दुख को आध्यात्मिक बना दो, ताकि व्यवस्था से कोई सवाल न पूछे। यह ‘पवित्रता की राजनीति’ है जो हर त्रासदी में एक प्रतीक तलाशती है और जनता को उस प्रतीक के पीछे बाँध देती है। “धर्मग्रंथ नहीं जले — इससे यह साबित होता है कि विमान को भगवान उड़ा रहे थे और उन्हीं से टेक्निकल फॉल्ट हो गया।” या “वो धार्मिक पुस्तक जलती तो शायद नागर विमानन निदेशालय(डीजीसीए) को जवाब देना पड़ता, अब जवाब तो ईश्वर ही देंगे।” इसीलिए, धर्म जब विवेक के साथ हो, तो वह मोक्ष की ओर ले जाता है। लेकिन जब वह अंधविश्वास के साथ हो, तो वह हमें विमानों के मलबे में ‘ईश्वर की सेल्फी’ ढूँढने वाले प्राणी बना देता है। ✍️ धर्म की वास्तविक महिमा तब होगी जब हम उसकी शिक्षा को बचाएँ — न कि उसके पन्नों को। जब अगली दुर्घटना हो — और होगी, अगर व्यवस्था यूँ ही लापरवाह रही — तो पवित्रता की तलाश मलबे में नहीं, जिम्मेदार संस्था/व्यक्ति की गर्दन पर होनी चाहिए।

भाग्य नहीं, व्यवस्था दोष है — संत्रास — एक विश्लेषण कि हम पीड़ित क्यों हैं और जिम्मेदार कौन है जब हम छुट्टी मनाने जाते हैं और आतंकी हमला हो जाता है, जब हम ट्रेन पकड़ते हैं और वह पटरी से उतर जाती है, जब हम फ्लाइट में चढ़ते हैं और वह क्रैश कर जाती है, जब हम हॉस्टल में खाना खा रहे होते हैं और प्लेन ऊपर से गिरता है— तब कोई यह कह देता है: हमारे हाथ में कुछ नहीं। बस कृपा यहीं रुक जाती है। ये जो शरीर की संरचना में सबसे ऊपर बुद्धि और विवेक का स्पेस है न इसकी कृपा। यह एक वाक्य नहीं, बल्कि एक पूरी पीढ़ी की चेतना को पंगु बनाने वाली विचारधारा है। मनोवैज्ञानिक आयाम: जब पीड़ा को सामान्य यानिकी ‘नॉर्मल’ बना दिया जाए तो मनुष्य बार-बार पीड़ा और असुरक्षा का सामना करता है, इस स्थिति में वह या तो विद्रोह करता है या फिर आत्मसुरक्षा के लिए मन को ‘संतुलित’ रखने हेतु उस दर्द को “भाग्य” कहकर स्वीकार करना शुरू कर देता है। इसे “Learned Helplessness” (प्रशिक्षित मजबूरी) कहा जाता है — जब व्यक्ति यह मान लेता है कि वह कुछ बदल नहीं सकता, तो वह प्रयास करना छोड़ देता है। यह एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, जिसे पहली बार 1960 के दशक में मनोवैज्ञानिक मार्टिन सेलिगमैन (Martin Seligman) ने प्रतिपादित किया था। वर्तमान के सोशल मीडिया दौर में यह भाग्यवाद दरअसल एक सामूहिक मानसिक रोग बन चुका है, जो व्यवस्था के असफलताओं को ‘प्राकृतिक आपदा’ में अनजाने ही बदल देता है। रेल/प्लेन दुर्घटना तकनीकी लापरवाही का परिणाम है, लेकिन मानसिक ढाँचा और सामूहिक चेतना बार बार यह दोहरा कर कहता है: “किस्मत में लिखा था”। नियति बनाम उत्तरदायित्व भारतीय दार्शनिक परंपरा में नियतिवाद की एक लंबी परंपरा रही है, परंतु उसके समांतर कर्मवाद और बौद्धिक आलोचना की धाराएँ भी विद्यमान रही हैं। लेकिन आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में जहाँ शासन, तकनीक और विज्ञान हमारी सुरक्षा के साधन हैं, वहाँ नियतिवाद का बढ़ा हुआ प्रभाव सत्ता की जवाबदेही से ध्यान हटाने का उपकरण बन चुका है। यह विचारधारा यह कहती है कि “दुर्घटना बस हो गई”, लेकिन कोई नहीं पूछता कि— • DGCA ने कितनी बार फ्लाइट की सुरक्षा रिपोर्ट को नजरअंदाज किया? • रेलवे ट्रैक का रखरखाव क्यों नहीं हुआ? • आतंकी हमले से पहले इंटेलिजेंस इनपुट को क्यों अनदेखा किया गया? 3. जब व्यवस्था खुद को ईश्वर बना ले जब समाज में संस्थाएँ—सरकार, कंपनियाँ, सुरक्षा एजेंसियाँ—अपने दायित्व से बचकर नागरिकों से सिर्फ धैर्य, सहिष्णुता और बलिदान की अपेक्षा करती हैं, तो वे खुद को एक प्रकार का ‘अप्रतिरोध्य देवता’ बना लेती हैं। यह प्रक्रिया जनता को “अ-राजनीतिक” बना देती है, जिससे वह न्याय की माँग नहीं करती, केवल श्रद्धा और समर्पण का भाव रखती है। इसका परिणाम यह होता है कि— • न्याय के लिए सड़क पर नहीं उतरा जाता, • जानने के हक का अभ्यास नहीं किया जाता। • कोर्ट में जनहित याचिक नहीं दायर होती। बल्कि केवल सोशल मीडिया पर मानसिक पंगुता के वाक्यों को दोहराया जाता है। सत्ता की जवाबदेही को धीरे-धीरे खत्म कर दिया जाता है? मीडिया और सांस्कृतिक विमर्श की भूमिका: शोक को साहस बनाकर परोसने का विकृत अभ्यास जब कोई बच्चा स्कूल की इमारत गिरने से मरता है तो न्यूज़ चैनल पर उसकी माँ के आंसू दिखाकर कहा जाता है: “ये माँ आज भी दूसरों के बच्चों को पढ़ा रही है, क्या अद्भुत जज्बा है!” लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि स्कूल की इमारत बिना मंजूरी के कैसे बनी? इंस्पेक्टर ने घूस लेकर आंखें क्यों मूंदी? शोक को “साहस” बना देना और दर्द को “संस्कार” बना देना एक गहरी विचारधारा का हिस्सा है— ताकि लोग कभी व्यवस्था से जवाबदेही न माँगें, केवल खुद को सुधारें। : हमें अपने डर और दुख से गुस्से तक की यात्रा तय करनी होगी जब तक हम “दुर्घटना” को भाग्य समझते रहेंगे, तब तक दोषी लोग अपराधों से बचते रहेंगे। जब तक हम सोचते रहेंगे कि “मरना तो एक दिन था ही”, तब तक व्यवस्था हत्यारी बनी रहेगी। सवाल करें, जवाब माँगें, और भाग्य की जगह व्यवस्था का उत्तरदायित्व तय करें। — अगर व्यवस्था ने असफलता की है तो हम ‘दुर्घटना’ के नहीं, ‘हत्या’ के शिकार हैं। यह प्रयास होगा पीड़ित को और अधिक पीड़ित बनाए बिना, उसके भीतर न्याय की मांग को पुनर्जीवित करने से। एक आह्वान करिए खुद से की मानसिक, दार्शनिक और सामाजिक चेतना की परतों को किसी भी सोशल मीडिया के भेड़चाल में धुंधला न होने देंगे।

विमान दुर्घटना के पीछे की अनदेखी: अहमदाबाद विमान दुर्घटना की दिल दहला देने वाली तस्वीरें और जानकारियाँ सामने आ रही हैं, और इसके साथ ही एक गहरी व शर्मनाक लापरवाही की कहानी भी उजागर हो रही है—एक ऐसी लापरवाही, जिसकी ज़िम्मेदारी सीधे तौर पर एयर इंडिया पर जाती है। न केवल DGCA (नागर विमानन महानिदेशालय) ने समय-समय पर चेतावनियाँ दी थीं, बल्कि एयरलाइन को कई बार शोकॉज़ नोटिस भी भेजे गए। अचानक हुए निरीक्षणों में भी विमान की सुरक्षा और कार्यक्षमता को लेकर गंभीर सवाल उठे थे। इन सबके बावजूद इन्हें नजरअंदाज़ किया गया। अब यह भी सामने आ रहा है कि एयरलाइन के CEO के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा—यह सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम की असफलता और मानवीय जीवन के प्रति असंवेदनशीलता का प्रतीक है। इस हादसे को और पीड़ादायक बनाता है एक और पहलू—यह कि एयर इंडिया अब भारत के सबसे सम्मानित और विश्वसनीय संस्थानों में से एक, टाटा समूह के स्वामित्व में है। ऐसे में सवाल उठता है: क्या रतन टाटा ने कभी ऐसी लापरवाही की इजाज़त दी होती? अगर उनके नेतृत्व में यह हादसा हुआ होता, तो क्या वे केवल बयान जारी कर चुप बैठ जाते? रतन टाटा जिस संवेदनशीलता, उत्तरदायित्व और नैतिक साहस के लिए जाने जाते हैं, अब वही आदर्श उनके समूह को अपनाना होगा। यह सिर्फ कॉर्पोरेट संकट नहीं है, यह नैतिकता का संकट है—एक संस्थान के आत्मसम्मान और जनविश्वास का संकट। एयर इंडिया के CEO कैम्पबेल विल्सन को अब पद से हटना ही होगा। उनके निर्णय—संभवतः मुनाफे की दौड़ में सुरक्षा को ताक पर रखना—241 ज़िंदगियाँ लील गया। यही निर्णय एयर इंडिया और टाटा ब्रांड की छवि पर हमेशा के लिए एक काला धब्बा बन गया है। इस भयानक हादसे में केवल एक व्यक्ति जीवित बचा है—अब वही जीवित गवाह है इस त्रासदी का। उसके शब्दों में वह सच्चाई होगी जिसे हम सबको सुनना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि जीवित बचा विवेक क्या कहेगा—सवाल यह है: क्या एयर इंडिया और टाटा समूह, सच में उस आवाज़ को सुनेंगे? क्या वे केवल मुआवज़ा देकर भूल जाने का रास्ता चुनेंगे, या आत्म-मंथन और उत्तरदायित्व का मार्ग अपनाएँगे? अब वक़्त है, कि आदर्शों की बात करने वाले, उन्हें जीकर भी दिखाएँ। अब वक़्त है, कि टाटा केवल एक ब्रांड नहीं, बल्कि एक ज़िम्मेदारी साबित हो।

अहमदाबाद विमान दुर्घटना: अधूरी उड़ानें, अनगिनत कहानियाँ अहमदाबाद में हुई विमान दुर्घटना महज एक किस्मत खराब होने की घटना नहीं है। तकनीकी असफलता भी इसमें थी— यह उन अनगिनत कहानियों का सामूहिक दुखांत है, जिन्हें शायद हम कभी जान भी न पाएँ। हर नाम, हर टिकट, हर सीट पर एक जीवन था—एक स्वप्न, एक मंज़िल, एक परिवार, एक भविष्य। एक परिवार सालों की तैयारी और संघर्ष के बाद अब इंग्लैंड बसने जा रहा था। कितने ही लोग पहली बार विदेश जा रहे होंगे, किसी बेहतर कल की तलाश में। कुछ ऐसे भी होंगे जो केवल लौट रहे थे—भारत दर्शन कर चुके विदेशी, या अपने घर लौटते प्रवासी। और क्रू? वे महज़ विमान परिचालक नहीं थे, वे भी किसी घर के कमाने वाले, किसी की माँ किसी के बेटे, किसी बच्चे के पिता, किसी भाई की बहन थीं। यह हादसा एक झटके में इन सभी कहानियों को अधूरा छोड़ गया। हमारे भीतर शोक है, लेकिन यह शोक मात्र आँसू नहीं—यह एक गहरी टीस है, उन आवाज़ों के लिए जो अब कभी नहीं सुनाई देंगी, उन यात्राओं के लिए जो कभी पूरी नहीं होंगी। इस त्रासदी ने एक बार फिर हमें झकझोर दिया है: शोक का समय है हम सब संत्रास में हैं पर फिर भी कुछ विचार होने ही चाहिए कि यह दुबारा न हो, कुछ सवाल कुछ चिंतन कुछ चेतना क्या हम अपनी व्यवस्थाओं में इंसानी जीवन की संवेदनशीलता को पर्याप्त महत्व दे रहे हैं? क्या सुरक्षा जांच के प्रति हम संवेदन शील है हमारी व्यवस्था संवेदन शील है? क्या उत्तरदायित्व की भावना अब केवल मुआवज़े और प्रेस रिलीज़ पर आकर सीमित रह जानी चाहिए? दुर्घटनाएँ केवल लोहे के टुकड़े और जले हुए ईंधन की कहानियाँ नहीं होतीं—वे उस सामाजिक और नैतिक गिरावट की भी कहानी होती हैं, जहाँ व्यवस्थाएँ जवाबदेही से मुँह मोड़ने लगती हैं। हम सिर्फ शोक न करें,सोचें उन सवालों पर जो तकलीफदेह तो हैं पर जरूरी हैं। जो लोग इस विमान में सवार थे, वे केवल यात्री नहीं थे—वे हमारे समय की संभावनाएँ थे। उनकी मौत केवल एक हादसा नहीं, हमारी व्यवस्थागत चूक का परिणाम भी है। हम हर बार की तरह चुप न रहें। हर उड़ान केवल उड़ान न हो—एक ज़िम्मेदारी भी हो। हर टिकट केवल यात्रा का दस्तावेज़ न हो—एक जीवन की गारंटी भी हो। यह सब उन लोगों के लिए जो उस दिन उड़ान भर रहे थे, अपने जीवन की किसी नई शुरुआत की ओर और उन सबके लिए भी, जो अब पीछे रह गए हैं—एक रिक्तता के साथ, जो कभी भरी नहीं जाएगी। मैंने देखा एक बूँद सहसा उछली सागर के झाग से रँगी गई क्षण भर ढलते सूरज की आग से। मुझको दीख गया : सूने विराट् के सम्मुख हर आलोक-छुआ अपनापन है उन्मोचन नश्वरता के दाग से! दिवंगत आत्माओं के लिए प्रार्थना श्रद्धांजलि🙏🏻🙏🏻

भारत की 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था — उपलब्धि की आधी कहानी भारत ने हाल ही में 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यह आंकड़ा न केवल भारत की वैश्विक आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि देश निवेश, उत्पादन और व्यापार के क्षेत्र में लगातार प्रगति कर रहा है। इस उपलब्धि को जापान को पीछे छोड़ने के रूप में प्रचारित किया गया, जिसने प्रतीकात्मक रूप से भारत को एशिया की प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया है। लेकिन जब इस आर्थिक सफलता की पड़ताल हम सामाजिक व मानवीय विकास के मानकों के आधार पर करते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि यह सफलता अधूरी है। आर्थिक विकास बनाम मानवीय विकास भारत की अर्थव्यवस्था का आकार बड़ा हुआ है, परंतु यदि हम इसे प्रति व्यक्ति आय और मानव विकास सूचकांक (HDI) के संदर्भ में देखें, तो तस्वीर पूरी तरह से अलग है। जापान को पीछे छोड़ देने के बावजूद, भारत जापान से जीवन गुणवत्ता के कई मामलों में दशकों पीछे है। प्रति व्यक्ति आय की विसंगति भारत की कुल GDP भले ही 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई हो, परंतु प्रति व्यक्ति आय अभी भी बहुत कम है — लगभग $2,500 प्रतिवर्ष। इसके मुकाबले जापान की प्रति व्यक्ति आय $40,000 से अधिक है। इसका अर्थ यह है कि भारत में आर्थिक विकास का लाभ बहुत सीमित वर्ग तक केंद्रित है। एक बड़े तबके के लिए यह ‘विकास’ केवल एक आंकड़ा मात्र है, जिसका उनके जीवन से कोई सीधा संबंध नहीं है। मानव विकास सूचकांक (HDI) की वास्तविकता मानव विकास सूचकांक तीन मुख्य क्षेत्रों को मापता है — जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और जीवन स्तर। • जीवन प्रत्याशा: जापान की औसत जीवन प्रत्याशा लगभग 84 वर्ष है, जबकि भारत की केवल 70 वर्ष के आसपास है। • शिक्षा: भारत में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच अभी भी असमान है, और उच्च शिक्षा में भी संसाधनों की भारी कमी है। • स्वास्थ्य सेवाएँ: भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली संसाधनों की कमी और कुप्रबंधन से ग्रस्त है, जिससे गरीब और ग्रामीण जनता बुरी तरह प्रभावित होती है। नीतिगत प्राथमिकताओं की खामी भारत की आर्थिक नीतियाँ मुख्यतः सकल घरेलू उत्पाद(GDP) वृद्धि पर केंद्रित रही हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे बुनियादी क्षेत्रों में अपेक्षित निवेश नहीं हो सका है। इस एकांगी सोच का परिणाम यह है कि देश की समृद्धि केवल कुछ शहरों और औद्योगिक केंद्रों तक सीमित रह गई है, जबकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में विकास की रोशनी अभी तक नहीं पहुँची। भारत में सामाजिक असमानता, बेरोजगारी, और खाद्य सुरक्षा जैसे मुद्दे अब भी गंभीर चुनौती बने हुए हैं। नीतिगत रूप से समावेशी विकास को प्राथमिकता न देने के कारण ही भारत आर्थिक आकड़ों में आगे होते हुए भी मानवीय विकास में पिछड़ रहा है। भारत का 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनना निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि है, लेकिन यह सफलता की आधी कहानी है। जब तक यह आर्थिक प्रगति आम नागरिक के जीवन स्तर को बेहतर बनाने में योगदान नहीं देती, और जब तक देश मानव विकास सूचकांक जैसे सूचकों पर वैश्विक मानकों के करीब नहीं पहुँचता, तब तक यह विकास अधूरा रहेगा। भारत को अब आवश्यकता है एक ऐसे दृष्टिकोण की, जो केवल आर्थिक वृद्धि पर नहीं, बल्कि समावेशी, न्यायसंगत और स्थायी विकास पर केंद्रित हो — जहाँ न केवल देश का आकार बड़ा हो, बल्कि हर नागरिक का जीवन भी बेहतर हो।

वट सावित्री व्रत: अध्यात्मिकता बनाम लोकबुझौन प्रियता – वट सावित्री व्रत, सावित्री-सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित एक लोक परंपरा है, जो स्त्री के पति-परायण धर्म, त्याग और आत्मबल को महिमामंडित करती है। यह पर्व स्त्री के उस संघर्षशील चरित्र का प्रतीक है, जिसमें वह पति की मृत्यु तक से संघर्ष करती है। किन्तु जब हम आज से लगभग 2500 से तीन हजार वर्ष पुराने इस आख्यान को वर्तमान समाज की कसौटी पर कसते हैं, तो कई प्रश्न उभरते हैं – क्या अब भी पति की सुरक्षा का उपाय उपवास और पूजन ही है? क्या यह व्रत आज भी उसी अर्थ में प्रासंगिक है, या यह अब केवल लोकबुझौन (लोकप्रियता के लिए किया जाने वाला सामाजिक आडंबर) बनकर रह गया है? ⸻ अध्यात्मिकता बनाम लोकबुझौन प्रियता व्रत-उपवास की परंपरा भारतीय संस्कृति में आत्मनियंत्रण और साधना का प्रतीक रही है। सावित्री की कथा में नारी का धैर्य, तप और विवेक एक अध्यात्मिक चरम की ओर संकेत करता है – जहाँ वह अपने ‘धर्म’ के बल पर मृत्यु जैसे प्राकृतिक नियम को भी चुनौती देती है। यह किसी स्त्री की भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति की कथा है। परंतु आज का सामाजिक परिप्रेक्ष्य इस आध्यात्मिकता से बहुत हद तक विचलित हो चुका है। व्रत की आंतरिक साधना की जगह बाह्य प्रदर्शन, वस्त्र-आभूषण, सोशल मीडिया पर तस्वीरें और सामूहिक आयोजनों ने ले ली है। यह रूप अधिकतर ‘लोकबुझौन प्रियता’ का परिचायक है – जहाँ परंपरा का पालन आत्मिक श्रद्धा से अधिक सामाजिक मान्यता और ‘कृत्रिम संस्कारबोध’ के तहत किया जाता है। ⸻ समाज में परिवर्तन और स्त्री की भूमिका 2500 वर्षों में भारतीय समाज में गहरे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आए हैं। आज की स्त्री शिक्षा प्राप्त है, आत्मनिर्भर है, और पारिवारिक के साथ-साथ सामाजिक-राजनीतिक जीवन में भी सक्रिय है। अब वह केवल ‘पति की छाया’ में रहने वाली पत्नी नहीं, बल्कि परिवार की समान भागीदार है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या आज भी पति की दीर्घायु और सुरक्षा का उपाय केवल स्त्री के व्रत और पूजा में निहित होना चाहिए? या फिर अब पारिवारिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, संवाद, सहयोग और समानता पर आधारित संबंध अधिक प्रासंगिक हैं? सावित्री के युग में स्त्री के पास शायद विकल्प सीमित थे; उसका साधन आस्था था। पर आज की स्त्री के पास विकल्प और स्वतंत्रता दोनों हैं। इसलिए अब केवल पूजा-पाठ से अधिक आवश्यक है कि पति-पत्नी दोनों एक-दूसरे के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक स्वास्थ्य की जिम्मेदारी बराबरी से उठाएं। व्रत का सामाजिक पुनर्पाठ यह आवश्यक नहीं कि वट सावित्री व्रत को त्याग दिया जाए, पर यह आवश्यक है कि हम इसके अर्थ को पुनर्परिभाषित करें। सावित्री केवल एक पतिव्रता स्त्री नहीं, वह न्याय के लिए लड़ने वाली, मृत्यु से डर न खाने वाली, और तार्किक संवाद करने वाली स्त्री है। यदि हम इस व्रत को केवल उपवास तक सीमित कर देते हैं, तो हम सावित्री की आत्मा से ही वंचित रह जाते हैं। आज का समाज तकनीकी, चिकित्सकीय और सामाजिक रूप से विकसित हो चुका है। पति की दीर्घायु अब आस्था और उपवास से अधिक, जीवनशैली, भावनात्मक संवाद, और समान सहभागिता से जुड़ी है। अस्पताल के खर्च, बीमा के प्रति जानकार होना, शिक्षा के माध्यम से जीवन रक्षा के उपायों के प्रति सजगता। आर्थिक रूप से सशक्त होने के उपाय करना। वट सावित्री व्रत का मूल्य अपडेट कर सकते हैं आज से यह तभी जुड़ेगा जब यह केवल एक रस्म नहीं, बल्कि स्त्री की चेतना, आत्मबल और विवेक का उत्सव बने। विवेकहीन होकर पेड काट कर उसकी डाल के सहारे रस्म अदायगी कितनी अध्यातमिकता है ? यह तभी अध्यात्मिकता के स्तर पर भी सजीव रहेगा जब आप आज की चुनोतियौं को समझेंगे।

“बुकर पुरस्कार और भारतीय भाषाएँ: अनुवाद के माध्यम से वैश्विक मंच पर साहित्यिक पुनर्जागरण” 2025 में कन्नड़ लेखिका बानू मुश्ताक की लघुकथा-संग्रह Heart Lamp को इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाना केवल एक साहित्यिक उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह भारतीय भाषाओं, विशेषकर कन्नड़ जैसी क्षेत्रीय भाषाओं के लिए एक सांस्कृतिक और भाषायी पुनर्जागरण की शुरुआत का प्रतीक है। पहले जब अनुवाद के माध्यम से हिंदी की रेत समाधि को यह पुरस्कार मिला तो यह घटना न केवल भारतीय साहित्य के लिए गौरव की बात रही, बल्कि वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में भाषायी विविधता के महत्व को रेखांकित करती हुई घटना साबित हुई। अब जब हर्ट लैंप को यह पुरस्करा मिला है तो हमें इसके अनुवादक को जानना चाहिए। हर्ट लैंप की अंग्रेज़ी अनुवादिका दीपा भास्थी ने मूल रचनाओं की आत्मा को न केवल भाषा में, बल्कि भाव, संवेदना और सामाजिक यथार्थ में भी ईमानदारी से रूपांतरित किया। यह उदाहरण दिखाता है कि अनुवाद केवल भाषाई हस्तांतरण नहीं है, बल्कि यह एक संस्कृति का एक दूसरी संस्कृति से संवाद है। अनुवाद के माध्यम से हाशिए की आवाज़ें, जो मुख्यधारा के विमर्श से अक्सर बाहर रह जाती हैं, अब वैश्विक पाठकों के समक्ष प्रस्तुत हो पा रही हैं। भारतीय भाषाओं की पुनराविष्कृति बहुभाषी भारत में साहित्य लंबे समय से क्षेत्रीय स्तर पर समृद्ध रहा है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेज़ी भाषा ने साहित्यिक प्रतिनिधित्व में प्रमुख स्थान घेर रखा था। हर्ट लैंप जैसी कृतियाँ और उनका सम्मान यह संकेत देते हैं कि अब हिंदी, कन्नड़, बंगाली, तमिल, मलयालम आदि भाषाओं का साहित्य भी वैश्विक मूल्यांकन और पाठकीयता का हिस्सा बन रहा है। इस नए युग में, भारतीय भाषाओं का साहित्य अब केवल “लोकल” नहीं रहा, वह “ग्लोबल” हो रहा है — पर शर्त यही है कि अनुवादक मूल रचना की चेतना को विश्व के संवेदनशील पाठकों तक पहुंचा सकें। साहित्यिक न्याय और प्रतिनिधित्व बानू मुश्ताक की कहानियाँ दलित, मुस्लिम, औरतों और गरीब तबके के जीवन की उन सच्चाइयों को उघाड़ती हैं, जिन्हें आमतौर पर साहित्य के सौंदर्यशास्त्र में ‘अप्रिय’ या ‘अनदेखा’ कहा जाता है। बुकर जैसी वैश्विक मान्यता यह दर्शाती है कि अब साहित्य में राजनीतिक चेतना, सामाजिक यथार्थ और भाषायी विविधता को नकारा नहीं जा सकता। यह एक साहित्यिक न्याय है — वह न्याय जो कहानियों, कविताओं और अनसुनी आवाज़ों को बराबरी का स्थान देता है। बुकर पुरस्कार का कन्नड़ साहित्य को मिलना, और उसके अनुवाद के माध्यम से विश्व-पटल पर पहुंचना, एक संकेत है कि यह भारतीय भाषाओं के लिए एक नया युग है — जहाँ वे न केवल अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखेंगी, बल्कि विश्व-साहित्य में निर्णायक हस्तक्षेप भी करेंगी। अब ज़रूरत है कि मराठी, उड़िया, असमिया और अन्य भाषाओं के सशक्त साहित्य को भी योजनाबद्ध तरीके से विश्वस्तरीय अनुवाद मिले, ताकि हर्ट लैंप की तरह अनेक “छिपे हुए दीपक” वैश्विक साहित्यिक आकाश में चमक सकें।

भारत में भाषाई व्यवहार और हिंदी की संपर्क भाषा के रूप में भूमिका: एक अनुभवजन्य विश्लेषण भारत की भाषिक संरचना विविध, बहुस्तरीय और ऐतिहासिक रूप से जटिल है। इस लेख में लेखक द्वारा भारत के विभिन्न क्षेत्रों—उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम—में निवास के दौरान देखे गए भाषाई व्यवहार के आधार पर यह प्रतिपादित किया गया है कि यद्यपि संविधानिक संरक्षण के तहत स्थानीय भाषाओं की प्रतिष्ठा बनी हुई है, परंतु प्रशासनिक और न्यायिक व्यवहार में अंग्रेज़ी का बढ़ता वर्चस्व क्षेत्रीय भाषाओं की प्रभावशीलता को सीमित कर रहा है। इस संदर्भ में हिंदी को एक संपर्क भाषा के रूप में—not as a national language but as a democratic link—विचार करने की आवश्यकता है। पंजाब राज्य का व्यवहारिक उदाहरण यह दर्शाता है कि स्थानीय भाषा संरक्षण और हिंदी के साथ संवाद, दोनों समानांतर रूप से संभव हैं। भाषिक विविधता और प्रशासनिक व्यवहार भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 भाषाओं के अतिरिक्त देश में हजारों बोलियाँ प्रचलित हैं। यद्यपि यह विविधता सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध करती है, परंतु प्रशासनिक, न्यायिक और अंतर-राज्यीय संवाद की दृष्टि से यह कभी-कभी बाधक भी बन जाती है। विशेष रूप से यह समस्या तब उभरती है जब स्थानीय भाषा न तो राज्य शासन के दस्तावेजों की भाषा बन पाती है, न ही उसे केंद्र के साथ संवाद का माध्यम बनने का अवसर मिलता है। इस स्थिति में दो मार्ग सामने आते हैं: या तो अंग्रेज़ी को सर्वमान्य संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार किया जाए, या फिर किसी भारतीय भाषा—जैसे हिंदी—को व्यवहारिक संपर्क भाषा के रूप में मान्यता दी जाए। यह लेख दूसरे विकल्प की व्यवहारिकता और औचित्य पर आधारित है। भारत के विभिन्न राज्यों में भाषाई व्यवहार: अनुभव आधारित अध्ययन दक्षिण भारत: हिंदी विरोध, परंतु अंग्रेज़ी पर निर्भरता तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में हिंदी के प्रति ऐतिहासिक राजनीतिक प्रतिरोध व्याप्त है। यह प्रतिरोध कभी-कभी सांस्कृतिक संरक्षण के नाम पर सामने आता है, किंतु व्यवहारिक रूप में न्यायिक और प्रशासनिक दस्तावेज़ अंग्रेज़ी में ही बनाए जाते हैं। किरायानामे, अनुबंध-पत्र, शपथपत्र, आवासीय प्रमाण आदि अंग्रेज़ी में होते हैं, जबकि स्थानीय भाषाओं का उपयोग केवल सीमित रह जाता है। यह विरोधाभास इस तथ्य को उजागर करता है कि स्थानीय भाषाओं के पक्ष में प्रतिरोध हिंदी के विरुद्ध होता है, परंतु परिणामतः अंग्रेज़ी को स्थायी स्थान प्राप्त होता है। उत्तर भारत: हिंदीभाषी क्षेत्र में भी अंग्रेज़ी की वर्चस्वता उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में हिंदी व्यापक रूप से बोली और समझी जाती है। किंतु न्यायिक क्षेत्र में उच्च न्यायालयों और ज़िला न्यायालयों में अंग्रेज़ी का ही प्रयोग होता है। अधिवक्ता और न्यायाधीश प्रायः दस्तावेज़ों को अंग्रेज़ी में तैयार करते हैं, जिससे आम जनता न्याय प्रक्रिया को समझने से वंचित रह जाती है। यह स्थिति दर्शाती है कि केवल हिंदीभाषी होना भी हिंदी के उपयोग की गारंटी नहीं है, और अंग्रेज़ी का औपचारिक वर्चस्व समान रूप से इन राज्यों में भी व्याप्त है। पंजाब: स्थानीय भाषा का व्यवहारिक प्रयोग और हिंदी के साथ सहअस्तित्व पंजाब में गुरुमुखी लिपि में पंजाबी भाषा का व्यापक और औपचारिक उपयोग होता है—चाहे वह किरायानामा हो या अदालत का दस्तावेज़। वहीं, हिंदी को सहज संपर्क भाषा के रूप में अपनाया गया है, विशेषतः केंद्र सरकार से संवाद के स्तर पर। पंजाब का यह मॉडल दर्शाता है कि स्थानीय भाषा के सम्मान और हिंदी के संवादात्मक प्रयोग के बीच कोई विरोध नहीं है। अंग्रेज़ी की आवश्यकता सीमित रह जाती है, और भाषाई संतुलन बनाए रखने की एक व्यवहारिक संभावना साकार होती है। हिंदी को संपर्क भाषा मानने के पक्ष में तर्क जनसांख्यिकीय विस्तार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 43% जनसंख्या हिंदी या उसकी उपभाषाओं को मातृभाषा के रूप में बोलती है। इस प्रकार हिंदी देश की सर्वाधिक व्यापक रूप से बोली जाने वाली भारतीय भाषा है। 2. भाषाई सुलभता और पारस्परिक समझ हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसे उत्तर, मध्य और पश्चिम भारत में सहजता से समझा जाता है। दक्षिण और उत्तर-पूर्व भारत में भी यह दूसरी भाषा के रूप में लोकप्रिय हो रही है, विशेषकर शहरी युवाओं और प्रवासी मज़दूरों के बीच। 3. अंग्रेज़ी पर निर्भरता: भाषाई विषमता का स्रोत अंग्रेज़ी का बढ़ता प्रयोग न केवल भाषाई असमानता उत्पन्न करता है, बल्कि स्थानीय भाषाओं के ह्रास का कारक भी बनता है। अंग्रेज़ी एक “आधिकारिक भाषा” बनकर जन-सामान्य को निर्णय-प्रक्रिया से दूर कर देती है। 4. प्रशासनिक समन्वय की आवश्यकता एक संघीय राष्ट्र में संपर्क भाषा की आवश्यकता प्रशासनिक समन्वय और नीति-निर्माण के लिए अपरिहार्य है। यदि यह भाषा हिंदी हो, तो संवाद अधिक सांस्कृतिक रूप से सन्निहित, सुलभ और सशक्त हो सकता है। ‘राष्ट्रीय भाषा’ नहीं, ‘संपर्क भाषा’ का विमर्श भारतीय संविधान ने किसी भी भाषा को ‘राष्ट्रीय भाषा’ घोषित नहीं किया है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा अवश्य दिया गया है, किंतु यह पद केंद्रीय प्रशासन तक सीमित है। ‘राष्ट्रीय भाषा’ की अवधारणा सांस्कृतिक असहमति को जन्म देती है, परंतु ‘संपर्क भाषा’ का प्रस्ताव प्रशासनिक और संवादात्मक आवश्यकता के रूप में सामने आता है। नीतिगत सुझाव 1. हर राज्य में स्थानीय भाषा को प्राथमिक प्रशासनिक और न्यायिक भाषा बनाया जाए, जैसा कि पंजाब में लागू है। 2. हिंदी को केंद्र-राज्य संवाद और अंतरराज्यीय संवाद के लिए संपर्क भाषा के रूप में उपयोग किया जाए, ताकि अंग्रेज़ी पर निर्भरता कम हो। 3. तीन-भाषा नीति को प्रभावी रूप से लागू किया जाए—मातृभाषा, हिंदी (या कोई अन्य भारतीय संपर्क भाषा) और अंग्रेज़ी, सभी को संतुलित रूप से सिखाया जाए। 4. स्थानीय भाषाओं में कानूनी साक्षरता अभियान चलाए जाएं, जिससे जन-सामान्य अपने अधिकारों को बेहतर समझ सके। भाषाओं का सहअस्तित्व भारत की लोकतांत्रिक शक्ति है, परंतु संवाद का साधन सभी के लिए समान और सुलभ होना चाहिए। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में अपनाना, यदि राजनीतिक रूप से संवेदनशील रूप में नहीं बल्कि व्यवहारिक नीति के रूप में किया जाए, तो यह न केवल अंग्रेज़ी के एकाधिकार को चुनौती देगा, बल्कि भारत की विविध भाषाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन देने का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। पंजाब इसका जीवंत उदाहरण है, जहाँ भाषिक अस्मिता और संवादात्मक व्यावहारिकता साथ-साथ चलती हैं। दक्षिण भारत के लिए यह एक नीतिगत प्रेरणा बन सकता है कि हिंदी को अस्वीकार कर अंग्रेज़ी को अपनाने से अच्छा है कि स्थानीय भाषा के साथ-साथ हिंदी को भी सम्मानपूर्वक अपनाया जाए, ताकि भारतीय भाषाओं का भविष्य सशक्त, स्वाभाविक और स्वतंत्र हो। संदर्भ 1. भारत सरकार (1963), राजभाषा अधिनियम 2. जनगणना 2011, भारत सरकार 3. पटनायक, डी. पी. (1990), Multilingualism in India, Multilingual Matters 4. अन्नामलाई, ई. (2001), Managing Multilingualism in India, Sage Publications 5. EPW Archives (1995–2020): भाषा नीति एवं प्रशासन पर लेख

फिल्म समीक्षा: ‘द डिप्लोमैट’ — नैतिक कूटनीति और भारत की वैश्विक छवि का सजीव चित्रण नेटफ्लिक्स पर हाल ही में आई फिल्म द डिप्लोमैट वास्तविक घटना पर आधारित केवल एक राजनीतिक थ्रिलर नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ सिनेमाई प्रस्तुति है जो भारत की नैतिक, व्यावहारिक और करुणा-आधारित विदेश नीति को ईमानदारी से प्रस्तुत करती है। ऐसे समय में जब सिनेमा अक्सर राजनीतिक लाभ या वैचारिक ध्रुवीकरण का माध्यम बन जाता है, द डिप्लोमैट एक संतुलित, संवेदनशील और ज़िम्मेदार कहानी के रूप में सामने आती है, जो स्वर्गीय सुषमा स्वराज जैसी नेतृत्वकर्ती की छवि को उजागर करती है। नैतिक कूटनीति: सुषमा स्वराज की विरासत इस फिल्म की सबसे सशक्त बात यह है कि यह दिखाती है कि कूटनीति केवल शक्ति नहीं, बल्कि सेवा और संवेदना का माध्यम भी है। स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज ने अपने कार्यकाल में इसी सिद्धांत को अपनाया था — चाहे वो विदेशों में फंसे भारतीयों को बचाने की बात हो, या सोशल मीडिया के ज़रिए सीधे नागरिकों से संवाद। द डिप्लोमैट इसी मानवीय दृष्टिकोण को सामने लाती है, यह दर्शाती है कि विदेश नीति केवल रणनीति नहीं, बल्कि एक नैतिक ज़िम्मेदारी है। यह भारतीय कूटनीति के उस पक्ष को उजागर करती है जिसे अक्सर नजरअंदाज किया जाता है — मूल्यों, संस्कृति और मानवीय गरिमा की रक्षा। सवाल उठाना, नफ़रत नहीं आप बिना नफरत फैलाये भी सही सवाल पूछ सकते हैं। जहां एक ओर केरला स्टोरी जैसी फिल्में राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विभाजन को बढ़ावा देने के लिए सायास प्रयास करती है और समाज को अतिरंजित पक्ष दिखाने के लिए आलोचवा का शिकार होती हैं, वहीं द डिप्लोमैट न केवल प्रणालीगत खामियों और नीति विफलताओं पर प्रश्न उठाती है, बल्कि ऐसा करते हुए किसी समुदाय, धर्म या देश को बदनाम नहीं करती। यह फिल्म तनाव नहीं, सोच उत्पन्न करती है। सिनेमा का असली उद्देश्य सवाल पूछना होता है, कटघरे में खड़ा करना नहीं। द डिप्लोमैट इसी संवेदनशीलता के साथ एक गंभीर संवाद की शुरुआत करती फिल्म है — सच के साथ, लेकिन संतुलन के साथ। भारत की असली छवि का प्रतिबिंब द डिप्लोमैट की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि यह भारत को किसी अतिरंजनात्मक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि एक यथार्थवादी, आलोचनात्मक और फिर भी राष्ट्रवादी नजरिए से दिखाती है। यह एक ऐसे भारत को दिखाती है जो लोकतांत्रिक मूल्यों, वैश्विक संवाद और ज़िम्मेदार निर्णयों में विश्वास करता है। यह फिल्म उस ‘सॉफ्ट पावर इंडिया’ की छवि को मजबूत करती है जो हिंसा या प्रचार से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता, विवेक और नैतिक नेतृत्व से दुनिया को प्रभावित करता है। : सिनेमा और विदेश नीति में एक नई दिशा द डिप्लोमैट, भारतीय सिनेमा के लिए एक नई दिशा तय करती है — जहां विदेश नीति केवल सत्ता का खेल नहीं, बल्कि एक नैतिक दायित्व के रूप में प्रस्तुत होती है। यह दिखाती है कि राष्ट्रहित और मानवाधिकार एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हो सकते हैं। सुषमा स्वराज जैसी नेत्री की तरह यह फिल्म भी एक ऐसी राह दिखाती है, जिसमें संविधान, करुणा और साहस तीनों का समावेश हो। आज के समय में, जब सिनेमा अक्सर विभाजन की दीवारें खड़ी करता है, द डिप्लोमैट संवाद की पुल बनाता है — और यही इसकी सबसे बड़ी सफलता है।