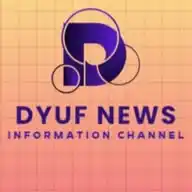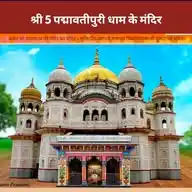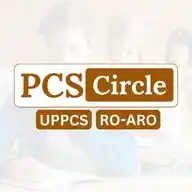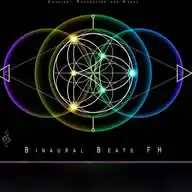'अपनी माटी' पत्रिका
815 subscribers
About 'अपनी माटी' पत्रिका
'अपनी माटी' पत्रिका के पाठकों हेतु समूह। नमस्कार। अन्य जरूरी प्रश्न हो तो 9116888201(Deepak) 9460711896(Manik)पर केवल वाट्स एप चैट सम्भव है। 'अपनी माटी' त्रैमासिक पत्रिका है इसके प्रत्येक वर्ष में चार सामान्य अंक 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर और 31 दिसम्बर को छपते हैं।।
Similar Channels
Swipe to see more
Posts

हिंदी भाषा और साहित्य की निर्मिति में राजस्थानी का विशिष्ट योगदान है। हिन्दी के ‘आदिकाल’ के परिसीमन में आने वाली ‘पुरानी हिन्दी’ की बहुत सी रचनाएँ आज प्राप्त हैं। वस्तुतः मैथिली को छोड़कर हिंदी परिवार की किसी भी भाषा की ऐसी कोई प्राचीन कृति सामने नहीं है, जिसके आधार पर आदिकाल का ढाँचा खड़ा किया जा सकता हो। केवल पुरानी राजस्थानी ही एक ऐसी भाषा है जिसका गद्य और पद्य दोनों प्रकार का साहित्य प्रभूत परिमाण में उपलब्ध है। राजस्थान के डिंगळ साहित्य में भारतीय संस्कृति, दर्प और शृंगार की अनेक अर्थच्छवियाँ मौज़ूद है। इतिहास पर दृष्टिपात करें तो स्वतंत्रता पूर्व राजस्थान 21 देशी राज्यों में विभाजित था। सर्वप्रथम जार्ज टॉमस ने इसे ‘राजपूताना’ कहा और तदनन्तर 1886 में कर्नल टॉड ने इस राज्य के इतिहास में इसे “राजस्थान”1 नाम दिया। यहाँ की भाषा और उसके इतिहास की बात करें तो राजस्थान के परगने और अनेक अंचलों में बोली जाने वाली बोलियों का अपना विशिष्ट साहित्य है। कहीं यह साहित्य वीरस्तुति काव्य (प्रशस्ति) के रूप में मिलता है, कहीं यह आध्यात्निक गलियारों से गुजरता है तो कहीं वेलि-ख्यात के रूप में तो कहीं यह अपने अनूठे प्रेमल स्वरूप में उपलब्ध है। राजपूताने में मेवाड़, मारवाड़, महोबा, चित्तौड़, बूँदी, जयपुर, नीमराणा, रीवा, पन्ना और भरतपुर राज्यों में विपुल मात्रा में चारण-साहित्य का रचाव हुआ। यद्यपि राजस्थानी साहित्य वीर-रस प्रधान है परन्तु भाषावैज्ञानिक अध्ययन करते हुए इसके प्रमाण में अन्य प्रवृत्तिगत साहित्य भी मुखर रूप से दिखाई देता है। राजस्थानी भाषा का अंश सिद्धों की उद्धृत रचनाओं में भी है, जिनकी भाषा को देशभाषा-मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी कहा गया, जो उस समय गुजरात-राजपूताना, ब्रजमंडल से लेकर बिहार तक पढ़ने-लिखने की शिष्ट भाषा थी। कबीर की साखियों की भाषा खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य ‘सधुक्कड़ी’ भाषा है। इस प्रकार राजस्थान में रचित साहित्य साहित्य की विविध प्रवृत्तियों को साथ लेकर चलता है। “राजस्थान का साहित्य विदेशी आक्रमण से देश, धर्म और जाति की रक्षा करने तथा संरक्षण के कर्तव्य के लिए असीम बलिदान करने की सक्रिय भावना से प्रारंभ होता है। इस भावना की अभिव्यक्ति की सारी प्रेरणा युद्ध, बलिदान तथा स्वधर्म के लिए सर्वस्व का उत्सर्ग कर देने की संस्कारगत उमंग से प्राप्त हुई है, अतः युद्ध की वीरोल्लासिनी हलचलों के बीच राजस्थान का साहित्य सारी जाति को त्याग और बलिदान का संदेश देता है।”2 वस्तुतः राजस्थान का इतिहास भारत की वीरता और जातीय अस्मिता का इतिहास रहा है। इसीलिए राजस्थान की महत्ता में आज भी यह गाया जाता है- *शोध आलेख : हिन्दी भाषा और साहित्य की निर्मिति में राजस्थानी का योग / विमलेश शर्मा* [ लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2025/03/blog-post_16.html ]


‘विमर्श’ शब्द अँग्रेजी के ‘डिस्कोर्स’ शब्द का पर्यायवाची है। जिसका अर्थ है- ‘संवाद’, ‘बहस’, ‘विचारों का आदान-प्रदान’ तथा ‘वार्तालाप’। किसी समस्या या स्थिति को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर जाँचने-परखने की प्रक्रिया विमर्श है। बीसवीं सदी में ‘वाद’ की लहर ऐसी उमड़ी थी कि हर चीज़ के पीछे ‘वाद’ को जोड़कर देखा जा रहा था, इक्कीसवीं सदी में ‘विमर्श’ शब्द की भी कुछ वैसी ही स्थिति बनी हुई है। स्त्री, दलित, आदिवासी, प्रवासी, पर्यावरण, थर्ड जेंडर, विकलांग, वृद्ध, बाल, किसान, मुस्लिम आदि विमर्श के केंद्र में आए हैं। इनकी छोटी-बड़ी समस्याओं, इनकी अस्तित्व-अस्मिता एवं इनसे जुड़े अहम सवालों को उठाने का कार्य साहित्य की विभिन्न विधाओं द्वारा किया जा रहा है। परिणामत: आज का साहित्य ‘विमर्शों का साहित्य’ की संज्ञा पाने लगा है। साहित्य विमर्श का मतलब है किसी रचना या साहित्य के बारे में गहराई से सोच-विचार करना और उसे समझने की कोशिश करना। साहित्य की अन्य विधाओं के मुक़ाबले जन-जन को आंदोलित एवं प्रेरित करने में कविता की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती है। [" शोध आलेख : 21वीं सदी की नेपाली कविता : विमर्शों की दशा एवं दिशा / गोविंद थापा क्षेत्री "अपनी माटी के इस आलेख को पूरा पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं ( अंक 57 ) ] लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2024/12/21_30.html

वैश्विक आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित है। कोविड 19 महामारी और वैश्विक स्तर पर जारी अन्य संकटों ने सतत् विकास लक्ष्य 3 की दिशा में प्रगति को बाधित किया है। बच्चों के टीकाकरण में पिछ्ले तीन दशकों में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई है। एक आंकड़े के अनुसार तपेदिक और मलेरिया से होने वाली मौतों में महामारी के पहले के स्तर की तुलना में वृद्धि हुई है।[1] भारत जैसे विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश में स्वास्थ्य एवं खुशहाली के मानवीय मुद्दे एक प्रमुख समस्या के रूप में विद्यमान है। यद्यपि भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। व्यक्ति के जीवन प्रत्याशा में वृद्धि हुई है, शिशु मृत्यु दर में कमी आई है लेकिन यह सुधार सभी के लिए समान स्वास्थ्य और खुशहाली में परिणित नहीं हुए हैं। विभिन्न क्षेत्रों, सामाजिक-आर्थिक समूहों, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी असमानताएं सर्वाधिक परिलक्षित होती हैं। 2022 के सतत् विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत 163 देशों में 121 वें स्थान पर है। [" शोध आलेख : सतत् विकास लक्ष्य 3 : चुनौतियां तथा भारत का प्रदर्शन / अजय कुमार यादव एवं सुनीता "अपनी माटी के इस आलेख को पूरा पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं ( अंक 57 ) ] लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2024/12/3.html

आजादी से ठीक पूर्व और आजादी के बाद राजस्थान से ठीक-ठाक संख्या में साहित्यिक पत्रिकाएँ निकालना प्रारंभ हो चुकी थी। इन पत्रिकाओं में धीरे ही सही मगर साहित्यिक आंदोलनों, घटनाओं एवं हिन्दी साहित्य के नव प्रयोगों के उतार-चढ़ाव दर्ज हो रहे थे। अगर राजस्थान से निकलने वाली लघु पत्र-पत्रिकाओं का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि 1880 से लेकर 2024 तक लगभग 100 से अधिक पत्र-पत्रिकाएँ निकल चुकी हैं।दशकवार भी देखें तो हर दशक में पांच-दस पत्रिकाएँ निकलती रहीं हैं। आज भी राजस्थान से 25 से 30 पत्रिकाएँ नियमित या अनियतकालीन निकल रही हैं । प्रारम्भिक पत्रिकाओं में ‘कलाधर’ (सं. मूलचंद भट्ट, पाली, 1949), ‘झरना’(सं. नेमीचंद्र जैन 'भावुक', जोधपुर, 1947), ‘राष्ट्रभाषा’ (सं. हरिप्रसाद शर्मा, जयपुर,1949), 'राष्ट्रवाणी' (सं. रामस्वरूप गर्ग, अजमेर,1949), 'किलकारी' (सं. दीपचन्द्र छंगाणी, जोधपुर,1949), 'साहित्य प्रवाह' (सं. नेमिचन्द जैन 'भावुक',जोधपुर,1950), 'प्रेरणा' ( सं. कोमल कोठारी,जोधपुर,1953), 'मरू भारती' ( सं. कन्हैयालाल सहल,पिलानी,1953) 'नवनिर्माण' (सं. नेमिचन्द जैन 'भावुक',जोधपुर,1953), 'राजस्थान साहित्य' ( सं.जनार्दन राय नागर,उदयपुर,1954), 'परम्परा' (सं.नारायण सिंह भाटी,जोधपुर,1956) आदि उल्लेखनीय नाम हैं। जब भी इस लघु पत्रिका आन्दोलन में'लहर' पत्रिका का जिक्र आता है तब अजमेर और प्रकाश जैन का नाम उभर कर सामने आता है लेकिन 'लहर' नाम सेपहली पत्रिका जोधपुर से निकली थी।महेंद्र मधुप के अनुसार – “राजस्थान की साहित्यिक पत्रिकाओं का आधुनिक काल जोधपुर से प्रकाशित होने वाली 'लहर' पत्रिका (1950) से होता है। इसके संपादक जगदीश ललवाणी और लक्ष्मीमल सिंघवी थे।”1 आलेख : राजस्थान की साहित्यिक पत्रकारिता और 'लहर' / माधव राठौड़ [ लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2025/03/blog-post_67.html ]


केदारनाथ सिंह की कविताओं में आरंभ से ही प्रकृति का आलंबन रहा है। वे अपने नन्हे से गुलाब के लिए सब्ज जमीन की तलाश करते दिख पड़ते हैं। केदारनाथ सिंह ने प्रकृति को – जैसा कि आरंभिक महाकाव्यों में प्रकृति को विभाव की कोटि में आलंबन मानकर किया गया वैसी आसक्ति से नहीं देखा है। प्रकृति से आलंबन का तात्पर्य है प्रकृति के उन तत्वों से जुड़ना जो हमारी भावनाओं, विचारों और अनुभवों को प्रभावित करते हैं। यह प्रकृति के सौंदर्य, शांति और जीवनदायिनी शक्ति से जुड़ने की प्रक्रिया है। आलंबन के अर्थ में पेड़-पौधे, पशु-पक्षी, नदी, समुद्र, झील, पहाड़, घाटियाँ, सूरज, चंद्रमा, तारे, हवा, बारिश और मौसम ये सभी आते हैं । इसके जुड़ने से हमें अपने जीवन में संतुलन, शांति और सुख की भावना मिलती है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और उसके साथ जुड़ने में मदद करता है, और हमें अपने जीवन को अधिक अर्थपूर्ण और सार्थक बनाने में सहायता करता है। केदारनाथ सिंह की बेचैनी और छटपटाहट इस दुनिया की या यूँ कहें कि ब्रह्मांड की मरम्मत करने की जुगत में है। उनकी कविताओं में पृथ्वी को बचाने की उद्दाम लालसा है। वे बाघ, सारस, कुत्ता-कुतिया, बैल, कौआ, गिलहरी आदि के प्रति ही अपनी जागरूक चेतना का उल्लेख नहीं करते, अपितु जीव अस्तित्व के आसन्न संकट के बोध को झरनाठ बरगद, घास, महुआ, मकई, नदी, पानी, आलू, धान, दाने आदि में भी संवेदना व्यक्त करते हैं । [" शोध आलेख : केदारनाथ सिंह के काव्य में मानवेतर प्राणी और उसकी संवेदना / रजनीश कुमार "अपनी माटी के इस आलेख को पूरा पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं ( अंक 57 ) ] लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2024/12/blog-post_604.html

आज़ादी के बाद से ही हमारा देश पुनर्निर्माण की प्रक्रिया से लगातार गुज़र रहा है। इस पुनर्निर्माण की प्रक्रियाएँ कागजों में बनाई तो जाती हैं लेकिन देश की एक बड़ी आबादी तमाम बुनियादी सुविधाओं से आज भी वंचित है। देश के तमाम बच्चे, बुजुर्ग, स्त्रियाँ, सामान्य जन सभी अपने अधिकारों के लिए शासन की ओर कातर दृष्टि से देखते रहते हैं। बाजारवाद, पूंजीवाद के प्रभाव में अमीर वर्ग निरंतर अमीर और गरीब वर्ग निरंतर गरीब होता जा रहा है। गरीब, वंचित समुदाय के लोगों के पास मंहगे प्राइवेट स्कूलों और अस्पतालों को देने के लिए फीस ही नहीं होती है तो वो उनकी सुविधाएं कैसे उठा सकेंगे। कहना ना होगा कि इन सबके साथ ही पूंजीवाद और बाजारवाद ने हमारी प्रकृति और हमारे पर्यावरण को भी हमसे छीनना शुरू कर दिया है। शहरीकरण की प्रक्रिया ने हमारी नदियों को हमसे छीन लिया है। सरकार नदियों के संरक्षण एवं उनके पुनर्जीवन के लिए हर साल लाखों करोड़ का बजट ले आती है। लेकिन नदियों की अवस्था में कोई सुधार होता नहीं दिख रहा। मलबों, कचरों और गंदे पानी से भरे सीवेज हमारी नदियों में सीधे गिरते हैं। कुछ जगहों पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए गए हैं जो कि इन नदियों को प्रदूषित होने से रोकने में नाकाफी हैं। देश की कई सारी नदियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, न जाने कितनी ही नदियों का पानी प्रदूषण के कारण काला हो गया है। ऐसी स्थिति में हमें इन नदियों के बचाने के बारे में गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। ये सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि सरकार द्वारा इन नदियों के संरक्षण एवं उनके पुनर्जीवन के लिए निर्धारित बजट का सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा है। [" शोध आलेख : कविता, नदी एवं जीवन की गतिमयता : राकेश कबीर की कविताएँ / अनिरुद्ध कुमार "अपनी माटी के इस आलेख को पूरा पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं ( अंक 57 ) ] लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2024/12/blog-post_779.html

पिछली शताब्दी के पहले दशक में कार्टून बनाने और छपने की रियाजात के बारे में हम बहुत थोड़ा ही जानते हैं। मसलन, हमें सरस्वती संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में यह जानते हैं कि वे कार्टून की संकल्पना विस्तृत ब्योरों के साथ लिखकर अपने प्रेस के अनुबंधित कलाकारों को देते थे। संपादक माँग के अनुसार कलाकार कार्टून बनाता था (सिंह 1951)। यह परंपरा बाद के दशकों में भी जारी रही, किन्तु साथ ही साथ तीसरे दशक से कार्टूनकार ख़ुद ही कार्टून बनाकर अपनी इच्छानुसार पत्रिका या संपादक को अपनी कला का नमूना भेजने लगे। मोहनलाल के उपलब्ध पत्रों से पता चलता है कि वह एक स्वतंत्र कार्टूनकार थे जो बाद में हिंदी पत्रिकाओं में कहानी, कविता, आलोचना, आदि भी लिखने लगे थे। उनके लिए, कार्टून बनाना हिंदी के खाली भंडार भरने के व्यापक राष्ट्रवादी परियोजना का हिस्सा था। वह ऐसे कलाकार नहीं थे जो किसी विशेष पत्रिका की संपादकीय टीम में कलाकारी करने, चित्र या कार्टून बनाने के लिए नियुक्त किये गए थे। उन्होंने संपादक की माँग पर कभी कार्टून नहीं बनाए। अलबत्ता, उन्होंने अपना कार्टून स्केच बनाकर इच्छुक संपादकों को प्रकाशित करने के लिए कहा। सकारात्मक उत्तर मिलने पर वे उन्हें अपनी टिप्पणी के साथ प्रकाशित करने के लिए भेजते। कम से कम उनके शुरुआती करियर को देखते हुए ऐसा ही लगता है। हालाँकि, उन्हें अपने कार्टून के लिए मिलने वाले पारिश्रमिक के बारे में हमें ठीक-ठीक नहीं पता। अपने वरिष्ठ मित्र और संपादक शिवपूजन सहाय को लिखे उनके पत्रों से जो पता चलता है वह है कि उन्हें अपने कार्टूनों के लिए पैसे मिलते थे जो उन्हें वैल्यू पेएबल पोस्ट (वीपीपी) से भेजे जाते थे। गंगा के संपादक शिवपूजन सहाय को लिखे एक लंबे पत्र से एक अंश ग़ौरतलब है। [" शोध आलेख : एक विस्मृत कार्टूनकार : मोहनलाल महतो ‘वियोगी’ (1901-1990) / प्रभात कुमार "अपनी माटी के इस आलेख को पूरा पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं ( अंक - 59 ) ] लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2025/03/1901-1990_31.html

अपने आरंभिक समय से ही सिनेमा विशेषकर हिंदी सिनेमा फ़ॉर्मूलाबद्ध रहा है यानी फिल्मों में जब कोई एक स्टोरी, हीरो-हीरोइन,चरित्र नायक-नायिका हिट हो जाया करते, निर्माता निर्देशक बार-बार उन्हें दोहराते रहते। ये स्टीरियोटाइप छवियाँ दर्शकों को भी लुभाती थी, वे मानाने को तैयार नहीं कि नायक ढिशुम-ढिशुम न करे या जिस कलाकार ने एक बार बहन की भूमिका निभा ली, दर्शक उसे नायिका यानी हीरोइन के रूप में कभी स्वीकार नहीं करेंगे, फिल्म का सुखांत, विवाह की शहनाई के साथ अंत यही मुख्य था। निर्माता जोखिम नहीं उठाना चाहते थे क्योंकि फ़िल्मों के फ्लॉप होने का ठप्पा यानी करियर खत्म ! लेकिन समय के साथ-साथ नए निर्देशकों ने जोखिम उठाना शुरू किया दर्शकों के मनोरंजन की भूख भी नए स्वाद की माँग करने लगी। आज लगभग एक शतक से अधिक समय पूरे कर चुका हिन्दी सिनेमा आज तकनीक और दर्शक केन्द्रित बन रहा है, सिनेमा के विकल्पों ने, तौर तरीकों ने बड़े-बड़े बैनरों को विवश किया कि वे अब दर्शकों को मूर्ख न समझे, जैसे कि कहा जाता था कि फ़िल्म देखने के लिए दिमाग घर पर रख कर जाओ! इस शोध आलेख में सिनेमा में हो रहे नवाचारों के विविध पक्षों को दिखाया गया है। *शोध आलेख : हिन्दी सिनेमा में नवाचार के विविध पक्ष / रक्षा गीता* [ लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2024/12/blog-post_248.html ]
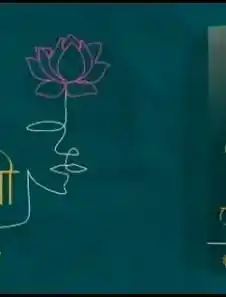

समाज और सिनेमा दोनों ही एक-दूसरे को विभिन्न पहलुओं में प्रभावित करते हैं। समाज का ही एक व्यक्ति फिल्मों में किरदार के रूप में नज़र आता है तो दूसरी ओर वही किरदार समाज के कई हिस्सों में पैदा होने लगते हैं क्योंकि सिनेमा समाज के युवा वर्ग के लिए एक रोल मॉडल प्रस्तुत करता है। प्रत्येक किरदार के कई पक्षों को सिनेमा में देखा जाता है परंतु जब नायक ही खलनायक के तौर पर नज़र आता है तो उसके हेयरस्टाइल और पहनावे से लेकर उसके विचार और डाइलोग्स, जनता को अधिक उत्तेजित करने लगते हैं। सिनेमा में समाज को एक नवीन दृष्टिकोण प्रदान करने की क्षमता है और फिल्मों का अभिनेता उस नवीन दृष्टिकोण को प्रदर्शित करने का एक सशक्त माध्यम हो सकता है। 21वीं सदी के सिनेमा के नायक जब एंटी हीरो या एक विलेन के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं तो यह भविष्य के लिए घातक सिद्ध होने की संभावना को बढ़ा देता है। प्रस्तुत लेख में हिन्दी सिनेमा में नायकों और खलनायकों के बदलते स्वरूप और जनता में उसके प्रभाव एवं आम जनमानस के मूल्यों में आए परिवर्तन को दर्शाने का प्रयास किया गया है। *शोध आलेख : हिन्दी सिनेमा में एंटी-हीरो और ट्रैजिक-हीरो की बढ़ती प्रवृत्ति / प्रिया कुमारी* [ लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2024/12/blog-post_235.html ]


शोध कार्य का मूल उद्देश्य मुस्लिम समुदायों की लड़कियों की शिक्षा तक पहुँच की समकालीन वास्तविकता की जाँच करना है। ताकि उनकी शैक्षिक स्थिति में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से उनकी समस्याओं तथा नीति एवं कार्यक्रमों को अमल में लाने के लिये सुझाव दिए जा सकें। इनमें मुस्लिम समुदायों की लड़कियों के तीखे पूर्वकालीन भेदों को, सामाजिक, आर्थिक परिवर्तन के जरिये काफी हद तक हल कर दिया गया है और इन्हें एक बेहतर सामान्य आधार प्रदान किया है। हालाँकि अभी भी बहुत हद तक भौतिक तथा सांस्कृतिक विभिन्नताएं बनी हुई हैं, फिर भी प्रासंगिक संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए इनकी शैक्षिक स्थिति को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। किसी आम भारतीय नागरिक की तरह हम जानते हैं कि ‘धर्म’ एक महत्वपूर्ण संस्था है। मुस्लिम धर्म कई वर्षों से भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का एक हिस्सा है परंतु इक्कीसवीं सदी में रहने वाले किसी भी भारतवासी की तरह हम यह भी जानते हैं कि ‘धर्म’ केवल हमारी मान्यता का नहीं बल्कि हमारे समाजीकरण का भी प्रभावी घटक है। यह ‘धर्म’, एक जो भारत के अतीत का हिस्सा माने जाते हैं और दूसरी जो कि भारत के वतर्मान का भी हिस्सा है, कहाँ तक समान हैं? इन विचारों को भी, इस अध्ययन में समझने का प्रयास किया है। [" शोध आलेख : मुस्लिम लड़कियों की शिक्षा : एक पुनरुत्पादित लोकाचार / वीरेंद्र कुमार चंदोरिया एवं पूजा सिंह "अपनी माटी के इस आलेख को पूरा पढ़ने के लिए दिए गए लिंक पर जाएं ( अंक 57 ) ] लिंक 👉 https://www.apnimaati.com/2024/12/blog-post_646.html